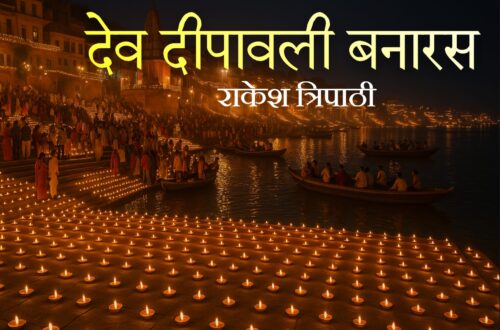सौरभ मेहता
भाग १
शहर की उस पुरानी गली में जहाँ मकानों की छतें एक-दूसरे के कंधे पर टिकी होती हैं और गलियों की साँसें भी धीमी पड़ चुकी होती हैं, वहीं तीसरे नंबर का मकान सबसे चुप है। दीवारों की सीलन अब तस्वीरों के किनारों तक पहुँच चुकी है, और खिड़कियों से झाँकती धूप ऐसी लगती है मानो किसी ने अनजाने में दरारों के बीच से उजाला गिरा दिया हो। उसी मकान की दूसरी मंज़िल की एक खिड़की, दोपहर के ठीक बीच में खुलती थी—बिना आवाज़ के, बिना किसी आहट के। और उस खिड़की के पीछे बैठी थी—श्रीमती सावित्री कक्कड़, जिनकी उम्र का अंदाज़ अब सिर्फ़ उनकी चुप्पियों से लगाया जा सकता था।
सावित्री कभी स्कूल में हिंदी पढ़ाती थीं। उनके बोलने का ढंग ऐसा था कि लगता जैसे शब्द भी उनके होंठों पर ठहरने से पहले दो बार सोचते हों। पति के जाने के बाद और बेटे के विदेश बसने के बाद, उनका जीवन एकरस हो गया था—एक किताब की तरह जो आधी पढ़ी रह गई हो। लेकिन दोपहर की इस खिड़की से वह रोज़ बाहर झाँकती थीं। सामने की इमारत में नई किरायेदार आई थी—एक अकेली युवती, जिसकी आँखों में हमेशा एक थकी हुई बेचैनी रहती थी, जैसे नींद और जागने के बीच कोई अनकहा दुख छुपा हो।
सावित्री ने उसे कई बार देखा था—सुबह अपने बालों को बाँधते हुए, छत पर सूखते कपड़ों को समेटते हुए, या नीचे दुकान से दूध लाते हुए। लेकिन आज पहली बार, उस युवती ने ऊपर खिड़की की तरफ देखा था। आँखों से सीधा आँखों में। बिना मुस्कान, बिना संकोच। सावित्री को लगा जैसे समय का एक सूत खिंच गया हो, जो दोनों की उँगलियों के बीच कहीं अटका रह गया हो।
शाम को जब चाय बनाई, तो एक कप ज़्यादा बना डाला। आदतन नहीं, जान-बूझकर। वह कप वहीं खिड़की की चौखट पर रख दिया, जैसे कोई प्रतीक्षा करता है कि कोई आए और कहे—”क्या ये मेरे लिए है?”
लेकिन कोई नहीं आया। खिड़की की बाहर वाली दुनिया में वही सन्नाटा था, वही टूटी हुई दीवारों के पीछे छुपे हुए रहस्य।
रात में जब पंखा घूमता रहा और नींद की जगह सिर्फ़ स्मृतियाँ सिरहाने पर बैठी रहीं, तब सावित्री को बचपन की याद आई। जब उनकी माँ भी ऐसे ही खिड़की के पास बैठी रहती थी। “खिड़कियाँ औरतों की दुनिया का हिस्सा हैं,” माँ कहा करती थीं। “दरवाज़े तो मर्दों के लिए होते हैं—भागने के लिए, लौटने के लिए। लेकिन खिड़कियाँ—बस देखने के लिए होती हैं, देखने और समझने के लिए।”
अगले दिन, सावित्री ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। जिसके पहले पन्ने पर लिखा था—”सुनने से पहले समझो। समझने से पहले देखो। देखने से पहले ठहरो।” उन्हीं पन्नों पर अब वह उस युवती के बारे में लिखने लगीं। बिना नाम के। बस एक छाया, जो हर दिन थोड़ा और साफ़ होती जा रही थी।
और एक दिन, दोपहर की उसी खिड़की से, उसने देखा—युवती रो रही थी। छत पर नहीं, सीढ़ियों की कोने में बैठी हुई। उसके पास कोई नहीं था। लेकिन उसकी पीठ पर वह छाया थी, जिसे हम अकेलापन कहते हैं। सावित्री का मन किया—नीचे जाएँ, उसका कंधा थपथपाएँ। लेकिन उनके पैर वहीँ जड़ हो गए।
उन्हें फिर से चाय बनानी पड़ी। वही दो कप।
लेकिन इस बार, खिड़की के नीचे से आवाज़ आई, धीमी पर स्पष्ट—”क्या ये मेरे लिए है?”
भाग २
“क्या ये मेरे लिए है?” उस आवाज़ ने सावित्री को भीतर तक हिला दिया। जैसे बरसों से बंद कोई दरवाज़ा किसी ने एक पल में खोल दिया हो। उनके हाथ में पकड़ा कप काँप गया, और उन्होंने जल्दी से चौखट पर रखा दूसरा कप उठाया, खिड़की से झाँक कर नीचे देखा।
नीचे वही युवती खड़ी थी। एक हल्की हँसी, एक थकी हुई मुस्कान उसके चेहरे पर थी। सावित्री को नहीं पता चला कि उस मुस्कान में विनम्रता थी या आग्रह, लेकिन उसने सिर हिलाकर ‘हाँ’ कर दिया।
“तो मैं ऊपर आ जाऊँ?” युवती ने कहा।
सावित्री को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह अंदर आईं, दरवाज़ा खोला, और पहली बार किसी को अपने घर के उस हिस्से में आने दिया जहाँ वर्षों से सिर्फ़ दीवारें थीं। सीढ़ियों की खटखटाहट के साथ एक नयी उपस्थिति धीरे-धीरे उनके जीवन में प्रवेश कर रही थी।
“मैं जोया हूँ,” वह मुस्कराते हुए बोली, कप हाथ में लेते हुए। “आपकी खिड़की से हर दिन देखती हूँ। लगता था, कोई तो है जो देख रहा है, बिना पूछे, बिना बोले।”
सावित्री को उसके शब्दों में कोई बनावटीपन नहीं लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपने दुखों को लेकर शोर नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो हर बात में एक सच्चाई चुपचाप बहती रहती है।
“अंदर आओ,” सावित्री ने कहा। “खिड़की से देखना जितना आसान है, किसी के पास बैठकर चाय पीना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन शायद जरूरी भी।”
जोया ने चाय का पहला घूँट लिया और एक गहरी साँस छोड़ी। “आपकी चाय में घर की ख़ुशबू है। जैसे किसी ने माँ के हाथों से फिर से जीना सिखा दिया हो।”
उस एक वाक्य ने सावित्री के भीतर कुछ ऐसा खोल दिया, जो शायद बरसों से बंद था। उन्होंने अपनी डायरी की तरफ देखा, जो अब भी मेज़ पर खुली पड़ी थी। जोया ने भी उस डायरी पर नज़र डाली।
“क्या मैं पढ़ सकती हूँ?” उसने पूछा।
सावित्री ने सिर हिलाया। “अगर पढ़ पाओ, तो ज़रूर। ये लिखी है, लेकिन हर शब्द के पीछे एक चुप्पी है।”
जोया ने एक पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था—
“कभी-कभी हम जिनके साथ जीते हैं, उनसे ज़्यादा वो समझते हैं जो बस देख लेते हैं। बिना सवाल किए। बिना उम्मीद के।”
वह चुप हो गई। फिर कुछ क्षण बाद बोली, “क्या आपको कभी लगा कि कोई अजनबी भी आपका घर बन सकता है?”
सावित्री ने उसकी आँखों में देखा। “घर कोई जगह नहीं होता। वो वो क्षण होते हैं जहाँ तुम समझे जाते हो। और मैं शायद तुम्हें समझ रही हूँ।”
दोनों चुपचाप बैठ गईं। चाय ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बातचीत शुरू हो गई थी—बिना ज़्यादा शब्दों के।
जोया ने बताया कि वह एक पत्रकार थी, पहले मुंबई में काम करती थी। लेकिन कुछ हुआ, ऐसा जो उसने विस्तार से नहीं बताया, और वह सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गई। अकेली, थकी हुई, और जीवन से कुछ दूर।
“लोग कहते हैं कि भागकर जाने से कुछ नहीं बदलता,” जोया बोली, “लेकिन कभी-कभी भागना ही बचने का एकमात्र तरीका होता है।”
सावित्री ने समझा, कि इस लड़की ने जो खोया है, वह सिर्फ़ नौकरी या शहर नहीं था। शायद भरोसा, शायद प्यार, शायद ख़ुद को।
शाम हो चुकी थी। जोया उठी। “मैं चलती हूँ, आंटी। अगर कभी दोपहर की चाय में एक कप और हो तो… मैं आ जाऊँ?”
सावित्री ने हँसते हुए कहा, “अब से वो कप हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। लेकिन एक शर्त है—तुम खिड़की से नहीं, दरवाज़े से आओगी।”
जोया चली गई। खिड़की से बाहर अब अँधेरा उतर रहा था, लेकिन सावित्री के भीतर एक नई रौशनी जल चुकी थी।
रात को डायरी में उन्होंने लिखा—
“आज एक लड़की आई थी। नाम है उसका जोया। लेकिन नाम से ज़्यादा उसकी चुप्पियाँ बोलीं। मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। धीरे-धीरे, जैसे कोई कविता जिसे बरसों बाद समझा जाए।”
अगले दिन दोपहर फिर आई। खिड़की खुली। दो कप चाय तैयार। और दरवाज़ा भी खुला।
जोया आई। इस बार हाथ में एक पुरानी डायरी थी।
“मेरे पास भी कुछ है। अधूरा है, लेकिन शायद आप पूरा कर सकें,” उसने कहा।
सावित्री ने डायरी ली, और दोनों बैठ गईं। एक पुराने घर में, दो औरतें, जिनके नाम एक-दूसरे के लिए नहीं थे, लेकिन पहचान थी। बिना रिश्तों के रिश्ते।
भाग ३
सावित्री ने जोया की तरफ देखा, उसकी आँखों में कुछ ऐसा था जो किताबों में नहीं मिलता—जैसे कोई शब्द जो लिखा नहीं गया, पर हर पंक्ति के बीच साँस लेता हो। वह डायरी जोया ने उन्हें दी थी, उसकी जिल्द पुरानी थी, कोनों से फटी हुई, और कागज़ों पर उंगलियों के निशान साफ़ दिख रहे थे। सावित्री ने उसे धीरे-धीरे खोला, जैसे कोई पुराना संदूक खोलते समय डरता है कि कहीं अतीत की धूल आँखों में न भर जाए।
पहले पन्ने पर लिखा था—”मैंने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने आप से भी न छुपूँ।”
जोया चुप थी, लेकिन उसकी उंगलियाँ कप के हैंडल पर टिकी थीं, जैसे किसी किनारे को पकड़ रखा हो।
सावित्री ने पढ़ना शुरू किया—
“दफ्तर की वो दोपहर अभी तक ज़ेहन में जिंदा है। जब मेरी आवाज़ किसी ने चुरा ली थी। वो रिपोर्ट जो मैंने तैयार की थी, उसके नीचे किसी और का नाम था। और मैंने सिर्फ़ देखा, चुपचाप। मुझे लगता था, मेरी कलम मेरी है, मेरी मेहनत मेरी है—लेकिन उस दिन समझ आया कि औरत की पहचान सबसे पहले छीनी जाती है, और सबसे आख़िर में वापस मिलती है।”
सावित्री ने पन्ना बंद किया। उसने जोया की आँखों में देखा, जो अब कुछ भी नहीं छुपा रहीं थीं।
“तुमने किसी से कहा नहीं?” सावित्री ने पूछा।
जोया हँसी, पर वो हँसी मुस्कान जैसी नहीं थी—वो एक हारे हुए सिपाही की तरह थी, जो अपनी तलवार ज़मीन पर रख चुका हो। “किससे कहती? जो कहते, ‘चलो आगे बढ़ो’, या जो कहते, ‘यही दुनिया है’? या उनसे जो मुस्कुराकर कहते, ‘तुम जैसी लड़कियाँ तो ये सब झेलने के लिए ही बनी हैं’?”
सावित्री की आँखों में एक पुरानी आँच चमकी। उसे अपने कॉलेज का समय याद आया। जब प्राचार्य के कमरे में एक लड़का, जो शहर का नामी वकील का बेटा था, उसकी पीठ के पीछे आकर खड़ा हुआ था। बस खड़ा—not touching, not speaking—लेकिन इतनी नज़दीकी से कि साँस लेना मुश्किल हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा था। न प्राचार्य से, न सहेलियों से, न घर पर। बस चुपचाप अगले दिन नौकरी छोड़ दी थी।
“मैं समझ सकती हूँ,” सावित्री ने धीरे से कहा, “कभी-कभी चुप्पियाँ ही चीखों की जगह ले लेती हैं।”
जोया की आँखों से एक बूँद टपकी, चाय के कप में जा गिरी। “आप क्यों समझती हैं मुझे? हम तो दो अलग-अलग पीढ़ी के लोग हैं।”
“शब्दों की उम्र होती है,” सावित्री बोलीं, “दर्द की नहीं।”
फिर कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। दीवार की घड़ी की टिक-टिक और बाहर से आती कबूतरों की फड़फड़ाहट, जैसे उनके बीच की खामोशी को और गहरा बना रही थी।
“कभी-कभी सोचती हूँ,” जोया ने कहा, “कि क्या मैं कुछ और बन सकती थी? अगर मुझे डर न होता, अगर मैंने वो दफ्तर न छोड़ा होता, अगर मैं लड़ती, तो शायद आज…”
सावित्री ने उसकी बात बीच में रोक दी। “अगर तुमने वो सब नहीं किया होता, तो तुम आज ये डायरी नहीं लिख पातीं। और शायद मैं ये पढ़ नहीं पाती। और शायद हमारी यह मुलाक़ात भी न होती।”
जोया ने सिर झुका लिया। उसकी उँगलियाँ अब डायरी के एक कोने से खेल रही थीं, जैसे किसी भूले हुए खिलौने से।
“क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ… रोज़?” उसने पूछा।
“तुम्हारा घर है,” सावित्री बोलीं, “तुम आओ, और अगर चाहो, तो लिखो। मेरे पास बहुत कागज़ हैं, और बहुत चुप्पियाँ भी।”
अगले दिन जोया आई, उसके हाथ में एक खाली नोटबुक थी। पहली बार वह मुस्कराई थी, खुलकर। उसने खिड़की के पास अपनी जगह बनाई, और लिखा—
“जब पहली बार किसी ने मेरी कहानी पढ़ी, तो मुझे लगा कि मैं एक बार फिर जी रही हूँ। पर इस बार डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ।”
सावित्री उसे देखती रहीं। उनका घर, जो पहले एक पुरानी किताब की तरह था, अब एक जीवित कविता जैसा लगने लगा था।
सावित्री ने अपने पन्ने पलटे, और लिखा—
“कभी-कभी, ज़िंदगी हमें दोपहर की एक खिड़की देती है—जहाँ धूप भी आ सके, और कोई अजनबी भी, जो धीरे-धीरे अपना बन जाए।”
खिड़की के बाहर वही पुराना मोहल्ला था। वही धूल भरी छतें, वही सूनी गलियाँ। लेकिन अब हर चीज़ थोड़ी कम थकी हुई लग रही थी। जैसे किसी ने हर ईंट पर नाम न सही, पर एक कहानी जरूर लिख दी हो।
शाम को जोया उठी। जाते-जाते बोली, “कल एक इंटरव्यू है। पत्रकारों के लिए। फिर से कोशिश करने जा रही हूँ।”
सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया। “इस बार अपनी कलम को कसकर पकड़ना। और अगर कोई नाम चुराए, तो उसे अपने शब्दों से चीर देना।”
जोया हँसी। “आपका आशीर्वाद चाहिए, आंटी।”
“मेरा नहीं,” सावित्री बोलीं, “तुम्हारा आत्मविश्वास चाहिए तुम्हें। और वह अब लौट आया है।”
रात को, खिड़की के पास बैठकर, सावित्री ने चुपचाप रेडियो खोला। पुराना सा गाना बज रहा था—”जिंदगी के सफर में गुज़र जाते हैं जो मकाम…” और उनकी आँखें भर आईं। लेकिन ये आँसू दुख के नहीं थे। ये उन क्षणों के थे जब कोई औरत किसी और औरत की चुप्पी को सुन लेती है—बिना शब्दों के।
भाग ४
सुबह की धूप इस बार खिड़की पर कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। सावित्री ने पर्दा थोड़ा सरकाया और बाहर झाँका। सड़क पर वही दूधवाला था, वही अखबार फेंकने वाला लड़का, वही कबूतर जो दीवार की मुंडेर पर बैठकर सहमते सूरज को देख रहे थे। लेकिन उस सुबह में एक बेचैन इंतज़ार भी था—जोया के लौटने का।
कल रात तक वो यहीं थी। फिर कहा, “इंटरव्यू है। पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब डर नहीं लगता। लगता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, जैसे कोई मेरी खामोशी को समझता है।”
सावित्री को लगा था कि शायद जोया अब लौटेगी नहीं। जैसे अक्सर लोग अपने दुखों को किसी के सामने रखकर फिर भाग जाते हैं—डरते हैं कि वो दुख उनका नाम न ले लें, उनका पता न माँग लें। लेकिन कहीं न कहीं, उसके चेहरे की ठहरी हुई मुस्कान ने कुछ और कहा था—वापसी का वादा।
दोपहर होते-होते सावित्री ने फिर दो कप चाय बनाई। वही तुलसी की पत्ती वाली, थोड़ी सी अदरक वाली। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई, जैसे कोई भूली हुई याद लौट आई हो। और तभी दरवाज़े की घंटी बजी।
जोया थी। लेकिन इस बार उसकी आँखों में कुछ नया था। वो थकी नहीं थी। उसकी साँसें तेज़ थीं, पर घबराई नहीं थीं। उसने सावित्री को देखा, जैसे कोई लंबा सफर तय करके अपने घर वापस लौटा हो।
“मिल गया काम,” उसने कहा, हँसते हुए, “वो भी शब्दों से जुड़ा। एक ऑनलाइन महिला पत्रिका में—’खुद की आवाज़’ नाम है उसका। और उन्होंने मुझसे मेरी डायरी माँगी।”
सावित्री की आँखों में चमक आ गई। “तो अब तुम्हारे शब्द सिर्फ़ तुम्हारे नहीं होंगे—बहुतों के होंगे।”
जोया ने सिर हिलाया। “लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई। इस खिड़की से। इस चाय से। और आपसे।”
दोनों खिड़की के पास बैठ गईं। बाहर हवा चल रही थी, गर्म नहीं, ठंडी भी नहीं—बस वैसी जैसी तब चलती है जब किसी पुराने पन्ने को नया पाठक मिल जाए।
“मैं एक कॉलम लिखना चाहती हूँ,” जोया बोली, “हर हफ्ते एक ऐसी औरत की कहानी जो बोल नहीं पाई। लेकिन उसके पास कहने को बहुत कुछ था। और मैं चाहती हूँ, पहला कॉलम आपके बारे में हो।”
सावित्री चौंक गईं। “मेरे बारे में? मैं तो बस एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरी कहानी में ऐसा क्या है?”
“आपने सुना है,” जोया बोली, “बिना सवाल पूछे, बिना तर्क किए। और सुनना इस दुनिया का सबसे कमज़ोर होता हुआ गुण है।”
कुछ देर बाद जोया ने डायरी निकाली, वही जो अधूरी थी। अब उसके आखिरी पन्नों में सावित्री के शब्द भी थे। उसने एक पैराग्राफ पढ़ा—
“मुझे लगता था कि मेरी खामोशी मेरा अकेलापन है। लेकिन जब कोई और उसमें अपनी परछाईं देख ले, तब खामोशी भी साझा हो जाती है। अब लगता है कि मैं भी कहीं लिखी हूँ, किसी और की डायरी में।”
सावित्री को समझ नहीं आया कि ये उसकी खुद की पंक्तियाँ थीं, या जोया की—क्योंकि अब उनके शब्द एक-दूसरे में घुल चुके थे।
तभी जोया ने अपना बैग खोला और एक पुराना स्कार्फ निकाला। गुलाबी रंग का, थोड़ी सी फटी किनारी वाला।
“ये मेरी माँ का है,” उसने कहा, “वो कहा करती थीं कि हर औरत को एक चीज़ हमेशा साथ रखनी चाहिए जो उसकी जड़ें याद दिलाए। जब मैं भागकर यहाँ आई थी, तो सिर्फ़ यही साथ था। और अब मैं ये आपको देना चाहती हूँ।”
सावित्री ने स्कार्फ लिया, और उसे अपनी हथेली में मोड़कर रखा। “अब ये जड़ें हम दोनों की हैं।”
शाम ढल रही थी। सूरज अब खिड़की की कोने से हट चुका था, लेकिन उसकी थोड़ी सी गर्मी अभी भी चौखट पर थी।
“मैंने एक औरत के बारे में लिखना शुरू किया है,” जोया ने कहा, “जो हर दिन एक पुरानी खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन असल में वह खुद को ही खोज रही होती है। वह खिड़की उसका आईना है। और एक दिन, वह देखती है कि आईने में कोई और भी है—जो उसके जैसी ही टूटी है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही है।”
सावित्री हँस दीं। “वो तुम हो?”
“शायद,” जोया मुस्कुराई, “या शायद हम दोनों।”
रात को जब जोया चली गई, सावित्री ने अपने पुराने अलमारी से एक फाउंटेन पेन निकाला—जो उन्होंने अपने पति से शादी के दिन तोहफे में पाया था। बरसों से बंद था। स्याही थोड़ी सूख गई थी, पर कलम अब भी सही चलती थी।
उन्होंने एक नया पन्ना खोला, और लिखा—
“आज किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे लगा कि मैं पहली बार पुकारी गई हूँ। कभी-कभी नाम ज़रूरी नहीं होते—पर समझे जाना, सुने जाना, सबसे बड़ा उपहार होता है।”
सावित्री ने खिड़की से बाहर देखा। सामने की छत पर जोया अब भी बैठी थी, अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए। हवा उसके बालों को पीछे उड़ाकर ले जा रही थी। और उसकी मुस्कान—वो वैसी थी जैसे कोई सफर पूरा होने पर मिले, और फिर तुरंत एक नया रास्ता दिखाई दे।
सावित्री ने खिड़की धीरे से बंद की। इस बार अंदर की दुनिया ज़्यादा खुली हुई थी।
भाग ५
अगली दोपहर कुछ अलग थी। खिड़की खुली तो हवा में बारिश की गंध थी। सावित्री की उंगलियाँ खिड़की की लकड़ी पर चली गईं, जहाँ वक्त ने अपने हल्के-हल्के निशान छोड़ दिए थे। नीचे गली में कुछ बच्चे भीगते हुए कागज़ की नावें बहा रहे थे, और हवा में एक धीमा-सा सुर गूंज रहा था, जैसे कहीं कोई पुरानी रागिनी लौट आई हो। सावित्री को आज फिर वही इंतज़ार था—जोया का।
अब ये मुलाकातें एक आदत बन गई थीं, लेकिन आदत से ज़्यादा एक जरूरत भी। दोनों के बीच ऐसा कुछ था जिसे किसी भी रिश्ते का नाम नहीं दिया जा सकता था, फिर भी वो हर दिन एक नई परिभाषा लेता जा रहा था।
“बारिश में चाय नहीं बनी तो सब अधूरा लगता है,” जोया ने आते ही कहा, बालों से टपकती बूँदों को झटकते हुए।
“और तुम नहीं आई होती तो चाय फीकी लगती,” सावित्री ने हँसते हुए जवाब दिया।
दोनों खिड़की के पास बैठे। जोया ने अपना लैपटॉप खोला, और सावित्री ने चाय की केतली गैस पर चढ़ा दी।
“आज एक मेल आया,” जोया ने कहा, “एक महिला ने लिखा है कि मेरी डायरी पढ़कर उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। और उसने भी पहली बार अपनी बेटी से अपने कॉलेज के दिनों की बात साझा की।”
सावित्री ने मुस्कुराते हुए चाय कपों में डाली। “कभी-कभी जब हम अपनी कहानी सुनाते हैं, तो वो किसी और की हिम्मत बन जाती है।”
“हाँ,” जोया ने कहा, “पर क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी दोपहरें किसी और के जीवन का जवाब बन जाएँगी?”
सावित्री ने सिर झुका लिया। “नहीं सोचा था। लेकिन जब जीना बाकी न बचे, तो देने की आदत लग जाती है। मैंने बहुत कुछ खोया है, जोया। लेकिन अब लगता है, वो सब शायद खोना ज़रूरी था—ताकि ये पल मिल सके।”
जोया कुछ देर चुप रही। फिर बोली, “आपकी कहानी अब मेरी डायरी में नहीं, एक किताब में है। मैंने एक प्रस्ताव भेजा है—’दोपहर की खिड़की’ नाम से। आपकी बातें, मेरी लेखनी।”
सावित्री हँसी, पर उस हँसी में आश्चर्य भी था, डर भी। “मेरी ज़िंदगी एक किताब कैसे बन सकती है?”
“क्यों नहीं?” जोया ने कहा, “हर औरत की कहानी एक किताब होनी चाहिए। और हर किताब किसी को बदल सकती है।”
सावित्री ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब थम रही थी। सड़क पर कुछ बच्चे अब कीचड़ में खेल रहे थे। औरतें अपनी बाल्टियाँ लेकर पानी जमा करने आई थीं। वही रोज़ की ज़िंदगी, वही दोहराव। लेकिन इस बार कुछ नया था—जैसे इन सबके बीच उनकी कहानियों का भी कोई स्थान बन रहा था।
“जब किताब छपेगी,” सावित्री ने कहा, “तो क्या नाम बताओगी लेखक का?”
“हम दोनों का,” जोया बोली। “शब्द मेरे हैं, पर जीवन आपका।”
सावित्री ने उसकी ओर देखा। “और तुम?”
“मैं?” जोया ने थोड़ी देर सोचकर कहा, “मैं आपकी छाया हूँ। जो आपकी चुप्पियों को शब्दों में बदल रही है।”
उस शाम, जोया ने पहली बार सावित्री का हाथ थामा। जैसे कोई बेटी माँ का हाथ थामती है किसी भीड़ में, यह समझकर कि वही सबसे सुरक्षित जगह है।
“क्या आपके पास मेरी उम्र की कोई बेटी होती,” जोया ने धीमे स्वर में पूछा, “तो क्या आप उससे भी यूँ ही बात कर पातीं?”
सावित्री की आँखें भर आईं। “मेरे पास एक बेटी होती… अगर वक़्त ने उसे छीना न होता। जन्म से पहले ही चली गई थी। डॉक्टर ने कहा—‘बचा नहीं सके’।”
जोया के चेहरे पर चुप्पी आ गई। लेकिन उस चुप्पी में एक अपनापन था, एक स्वीकृति।
“तो अब मान लीजिए, आपकी बेटी हूँ,” जोया ने कहा, “और आप मुझे वही कह सकते हैं, जो आपने कभी अपनी बेटी से कहना चाहा हो।”
सावित्री ने उसकी तरफ देखा—कहीं कोई रक्त संबंध नहीं था, कोई सामाजिक मंज़ूरी नहीं, कोई नाम नहीं, कोई दस्तावेज़ नहीं—लेकिन फिर भी रिश्ता इतना गहरा था कि शब्द भी उसके सामने ठिठक जाते।
“तो सुनो,” सावित्री ने कहा, “जब भी लगे कि तुम्हारा रास्ता तुमसे छिन रहा है, तो उस खिड़की के पास आ जाना। और अगर मैं न भी रहूँ, तो ये खिड़की तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाएगी। यहाँ से जितनी धूप भीतर आई है, उतना ही विश्वास बाहर गया है।”
जोया की आँखों से दो बूँदें टपकीं। लेकिन इस बार वे आँसू नहीं थे—वे वचन थे।
रात जब ढल रही थी, सावित्री ने उस स्कार्फ को अपनी अलमारी में नहीं, सिरहाने पर रखा। और एक चिठ्ठी लिखी—
“मेरी सबसे प्यारी बेटी जो कभी जन्म नहीं ले सकी—आज मैं तुझे जोया के रूप में पा चुकी हूँ। तू अब शब्दों में है, धड़कनों में है, और सबसे ज़्यादा—खिड़की की उस दोपहर में है, जहाँ से ज़िंदगी फिर से मुस्कराई।”
भाग ६
खिड़की से झाँकती हुई उस दोपहर की धूप अब सावित्री के कमरे में एक और रंग ले आई थी—सुनहरा नहीं, थोड़ा गुलाबी, थोड़ा हल्का नीला। ऐसा रंग जो बदलते रिश्तों का होता है, जब कोई अनजाना अपना बन जाए, और अपना भी कुछ नया कह जाए।
जोया अब लगभग रोज़ आती थी। पहले सिर्फ़ दोपहर में, फिर कभी-कभी सुबह भी, और अब तो कुछ शामें भी यहीं बीतने लगी थीं। उसने खिड़की के कोने में एक छोटा सा गमला भी रख दिया था—उसमें मनी प्लांट की बेल जो सावित्री के कहने पर नहीं, बल्कि अपने मन से लाई थी। “हमारी खिड़की की हरियाली,” उसने कहा था, “जिसे कोई शब्द नहीं चाहिए, फिर भी वो बढ़ती रहती है।”
उस दिन भी वो आई। हाथ में किताब थी—छपी हुई, असली, कवर पर नाम लिखा था:
“दोपहर की खिड़की”
लेखिका: जोया खान एवं सावित्री कक्कड़
सावित्री को जैसे यक़ीन ही नहीं हुआ। उसने किताब को अपने हाथ में लिया, उंगलियों से उसके कवर को छुआ, जैसे किसी पुराने सपने को पहली बार ज़िंदा देखा हो। उसकी आँखों में एक ऐसा संतोष था जिसे शब्दों में बाँधना मुश्किल था।
“मैंने प्रकाशक से कह दिया था,” जोया बोली, “इस किताब का विमोचन यहीं होगा, इस खिड़की के पास। न कोई मंच, न कोई भाषण। बस कुछ चाय, कुछ यादें, और आप।”
सावित्री हँसी। “तुम्हें पता है, ये किताब अब मेरा नहीं रही। ये हर उस औरत की है जो बोल नहीं पाई, जो जीते-जी सिर्फ़ सहती रही, और फिर किसी खिड़की से अपनी कहानी सुनाई।”
जोया चुप रही। फिर धीमे से बोली, “आंटी, क्या कभी आपने किसी से प्रेम किया था? उस प्रेम के सिवाय जो शादी में बाँध दिया जाता है?”
सावित्री के हाथ काँपे। यह सवाल कोई आसान नहीं था, न सुनने के लिए, न जवाब देने के लिए। लेकिन जोया के साथ अब चुप्पी भी विश्वास बन गई थी।
“था एक,” सावित्री ने कहा, “कॉलेज के समय। उसका नाम था आदित्य। वो कविता लिखता था, और मुझे सुनाता था। कहता था, तुम मेरी कविता की आखिरी पंक्ति हो, सावित्री। पर फिर घरवालों ने रिश्ता तय कर दिया—शादी, बच्चे, नौकरी। आदित्य पीछे छूट गया। शायद इसीलिए मैं तुम्हें इतना समझती हूँ—मैंने भी अपने शब्द खोए थे।”
जोया ने सावित्री का हाथ थाम लिया। “शायद आपके शब्द अब लौट आए हैं, मेरी कलम में।”
उस शाम को जोया और सावित्री ने मिलकर पहली बार सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो किया। जोया की नई पत्रिका ने कहा था—”हम चाहते हैं कि लोग आपकी कहानी जानें।”
कैमरा ऑन हुआ। जोया ने मुस्कराकर कहा, “नमस्ते। आज आप सबसे मिलवा रही हूँ मेरी सबसे खास लेखिका से—सावित्री कक्कड़। उम्र पूछिए मत, क्योंकि कहानियों की कोई उम्र नहीं होती। और आज हम बात करेंगे ‘दोपहर की खिड़की’ की, एक ऐसी जगह जो खिड़की होते हुए भी दरवाज़ा बन गई।”
लाइव में हज़ारों दर्शक थे। सावित्री घबराई हुई थीं, पर उन्होंने जोया के कंधे को देखा, और धीरे-धीरे बोलना शुरू किया—
“मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी चुप्पियाँ किसी के लिए शब्द बन जाएँगी। लेकिन जोया आई, और उसने मेरी ज़िंदगी को दोबारा लिखा। हम सबके पास एक खिड़की होती है, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, पर बोलते नहीं। ये किताब उस पहली आवाज़ की तरह है, जो आप खुद के लिए निकालते हैं।”
लाइव ख़त्म हुआ। तालियाँ तो नहीं थीं, पर मोबाइल पर हार्ट और कमेंट्स की बाढ़ आ गई।
“आप मेरी माँ जैसी लगती हैं,” किसी ने लिखा।
“मुझे अब यक़ीन है कि मेरी कहानी भी सुनी जाएगी,” किसी और ने कहा।
जोया ने सब पढ़ा, और एक लंबी साँस ली। “आपने नहीं लिखा, आंटी। आपने सबका लिखा है।”
रात में जब जोया चली गई, सावित्री ने किताब को सिरहाने रखा। लेकिन उस रात उन्होंने जो सपना देखा, वो अलग था।
सपने में वही पुराना कॉलेज था, वही आदित्य, वही बरगद का पेड़। लेकिन इस बार वो कुछ कहने से पहले रुक नहीं गया। उसने सावित्री की तरफ देखा और कहा—”शब्द लौट आए हैं। अब डरने की ज़रूरत नहीं।”
सुबह उठकर उन्होंने डायरी में लिखा—
“मैं अब अधूरी नहीं हूँ। किसी ने मेरी चुप्पियों में पंक्तियाँ देखीं, किसी ने मेरी खामोशी से कहानी बुन ली। अब लगता है, मैं भी एक किताब हूँ—जिसका हर पन्ना धीरे-धीरे खुल रहा है।”
और खिड़की की उस दोपहर में अब धूप के साथ-साथ एक किताब भी थी—जिसमें सावित्री नहीं, हर स्त्री थी—अपने पूरेपन के साथ।
भाग ७
वर्षा ऋतु की अंतिम बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। सावित्री खिड़की के पास बैठी, अपने घुटनों को रेशमी शॉल से ढँककर बाहर झाँक रही थीं। अब यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था—हर सुबह खिड़की खोलना, धूप या बादल की परवाह किए बिना वही जगह पर बैठना, और अपने भीतर की आवाज़ों को सुनना। लेकिन आज एक अजीब बेचैनी थी, जैसे मन के किसी कोने में एक धूल भरी संदूक खुल गई हो।
जोया आज नहीं आई थी।
पिछले कुछ महीनों से जोया की उपस्थिति सावित्री की ज़िंदगी में वैसे ही हो गई थी जैसे दीवार पर चलती घड़ी—जिसके टिक-टिक से घर में जीवन की ध्वनि बनी रहती है। पर आज वह खामोशी थी।
उन्होंने फोन उठाया, लेकिन रुकीं। “उसे आज़ाद रहने दो,” उन्होंने मन में कहा, “शायद उसे आज अपने आप से मिलने की ज़रूरत है।”
इसी बीच डाकिया आया। पुराने ज़माने की आदत थी कि डाक की हल्की सी आवाज़ पर भी सावित्री का दिल धड़कने लगता था। दरवाज़े के पास पड़ी चिट्ठियों में एक लिफाफा था—जिसमें हाथ से लिखा हुआ पता था। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया।
आदित्य मुखर्जी
उनकी उँगलियाँ काँपने लगीं। लिफाफे को कई बार उलट-पुलट कर देखा, फिर धीरे-धीरे खोलने लगीं, जैसे कोई भूली हुई किताब का पन्ना पलटना हो।
“प्रिय सावित्री,”
“आज इतने वर्षों बाद ये चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। नहीं जानता कि तुम मुझे याद करती हो या नहीं, पर मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। वो कविता की पंक्तियाँ जो अधूरी रह गई थीं, वो सब तुम्हारे जाने के बाद हर रात मेरी डायरी में उतरती रही। मैंने सुना है, तुम एक किताब की लेखिका बनी हो। ‘दोपहर की खिड़की’—मैंने वो किताब पढ़ी, और हर शब्द में तुम्हारी आवाज़ पहचानी।”
“शायद अब देर हो चुकी है, लेकिन अगर कभी मिल सको, तो मैं बनारस में हूँ। घाट पर वही पुरानी चाय की दुकान अब भी चलती है। हर शाम वहाँ बैठकर वही कविता लिखता हूँ, जिसका आखिरी शब्द तुम थीं।”
“तुम्हारा—आदित्य”
सावित्री चुपचाप वहीं बैठ गईं। इतने वर्षों बाद, जैसे जीवन की किसी पुरानी गलती ने दरवाज़ा खटखटाया हो। लेकिन इस बार वह गलती नहीं लग रही थी—एक अनकहा संवाद था, जो वर्षों से अधर में लटका था।
शाम को जोया आई। उसके चेहरे पर थकावट थी, आँखों में कोई छुपा हुआ द्वंद्व।
“आज मैं नहीं आना चाहती थी,” जोया बोली, “पर पता नहीं क्यों, आपके बिना मन नहीं लगा।”
सावित्री ने चिट्ठी आगे बढ़ाई।
जोया ने उसे पढ़ा। फिर सावित्री की आँखों में देखा। “जाओगी?” उसने पूछा।
“नहीं जानती,” सावित्री ने उत्तर दिया। “वो एक बीता हुआ अध्याय है। और शायद अब मुझे किताब को बंद रहने देना चाहिए।”
“पर आपने ही सिखाया था कि अधूरी पंक्तियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं,” जोया बोली। “और शायद ये वही आखिरी वाक्य है, जो आपसे कहा जाना चाहिए था।”
रात को सावित्री ने पहली बार वर्षों बाद ट्रंक खोला। उसमें वही पुरानी साड़ी रखी थी—हल्के नीले रंग की, जिसके पल्लू पर आदित्य ने फूलों का चित्र बना दिया था कॉलेज के दिनों में। एक कविता की फटी कॉपी भी थी, और वह रुमाल जिसमें उनकी माँ ने पहली बार चूड़ियाँ बाँधी थीं।
उन्होंने वह साड़ी निकाली और सिरहाने रख दी। शायद कल वह ट्रेन पकड़ेंगी। शायद नहीं भी। लेकिन इतना तय था कि अब वह अपने अतीत से डर नहीं रहीं थीं।
“अगर मैं बनारस गई,” उन्होंने जोया से कहा, “तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी?”
जोया चौंकी। “मैं?”
“हाँ,” सावित्री ने मुस्कराते हुए कहा, “क्योंकि अब तुम सिर्फ़ मेरी कहानी की गवाह नहीं, उसका हिस्सा हो।”
जोया की आँखों में आँसू थे। “मैं चलूँगी। पर एक शर्त है—आपको वह कविता पूरी करनी होगी, जो आपने कभी आदित्य के लिए लिखी थी।”
सावित्री ने सिर हिलाया।
और उस रात, खिड़की के पास बैठकर, उन्होंने लिखा—
“तुम मिले नहीं, पर कहीं भी नहीं खोए
हर पन्ने पर तुम्हारी आहट थी
अब जब जीवन लौटने को कहे
मैं भी कहूँगी—हाँ, अब समय है।”
बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। लेकिन खिड़की की चौखट अब भी सूखी थी। क्योंकि भीतर की आँधी अब शांत हो चुकी थी।
भाग ८
बनारस के घाट पर पत्थर की वे सीढ़ियाँ, जहां गंगा जल हर शाम गुलाबी-नारंगी रंग लेता है, आज उसी रंग में सावित्री का इंतज़ार कर रही थीं। उनके हाथ में वह हल्की नीली साड़ी थी, जिसकी राखी हरी चुनर पर आदित्य ने कॉलेज के दिनों में तुलसी की पत्तियों से पुष्पांकित कविता लिखी थी। चाय की दुकान से आती मटमैली मिट्टी की खुशबू, मन्दिर की घंटियों का तान और हवा में झिलमिलाते क़रीबियों के दीपक — सब कुछ मानो पुराने वक्त को नए सिरे से इन्तज़ार में बंधा रहा था। सावित्री ने घाट की ओर देखा, जहां दूर से जोया तेज़ कदमों से आ रही थी, उसके हाथ में एक पुरानी कॉपी थी — जिस पर सावित्री की लिखी अधूरी कविता समायी थी।
जोया आकर खड़ी हुई और शोल्डर बैग से कॉपी निकालकर सावित्री को थमा दी। “यह आपका है,” उसने कहा, “जिसने दस साल तक अधूरे पन्नों में सांसें भरी थीं।” सावित्री ने कॉपी खोली और कोने में गिले-शिकवे से भरी पंक्तियाँ पढ़ीं: “तुम मिले नहीं, पर कहीं भी नहीं खोए / हर पन्ने पर तुम्हारी आहट थी / अब जब जीवन लौटने को कहे / मैं भी कहूँगी—हाँ, अब समय है।” यह शब्दों का सच था, उनकी अपनी आत्मा की आवाज़, जो अब पूर्ण होकर वापसी की राह देख रही थी। गंगा की लहरें उनके पैरों के पास सरकने लगीं, मानो सुन रही हों कि जीवन की अधूरी धुन अब मुकम्मल होने वाली है। सावित्री ने जोया की ओर देखा, आँखों में आभार के आँसू थे, लेकिन लबों पर मुस्कान भी थी, क्योंकि जोया वहाँ सिर्फ़ एक साथी नहीं, उनकी बेटी थी—वह जो नामों के बंधन से परे, अपूर्व विश्वास और साँझा समझ से जुड़ी थी।
एफ़साना देखकर घाट की स्याही और आसमान के बीच एक मध्यम निशान बन गया था जहाँ शाम की मंद रोशनी उतरती थी। अचानक दूर से एक साया दिखा — पतली चाल, धीमी मगर निश्चित। आदित्य था, जो वर्षों बाद वहीँ चाय की दुकान से ठंडा पानी पीता हुआ आया। उसके हाथ में एक गुलाबी गुलदस्ता था, मटर-गुलाबी रंग के फूल, जो किसी पर्व की खबर नहीं लाते, बल्कि प्रेम के सूखे किनारों को हरा-भरा कर जाते हैं। आदित्य का चेहरा समय की तहें खोले हुए था — कुछ झुर्रियाँ, कुछ चिरकुट दाढ़ी के निशान, लेकिन आँखों में वही नमकीन चमक थी, जो सावित्री की याद में कभी बुझी नहीं थी। उसने कदम बढ़ाए, लेकिन कोरी हवा से पहले जोया ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, “ये आपकी माँ हैं।” आदित्य ने हल्की झुककर सावित्री का अभिवादन किया, और वह क्षण कुछ और नहीं, बल्कि वर्षों की चुप्पियों का संगम था।
सावित्री ने अपना शॉल उतारा और धीरे-से अदित्य के कंधे पर डाल दिया, जैसे कह रही हो — “यह वही सिल्क है, जो उस दिन दिया था, जब तुमने पहली बार ‘साथ’ की परिभाषा बताई थी।” आदित्य ने हाथ में पकड़े गुलदस्ते की नाज़ुक कोंपलें सावित्री के सामने झुकाईं, “ये फूल शायद कविताओं की तरह सौम्य हों,” उसने कहा, “पर इनमें मेरी भूल-भुलैया की सारी खुशबू है, जहाँ मैं तुम्हें तलाशता रहा।” सावित्री ने गुलदस्ते को अपनी छाती के पास दिलाया, और उसकी आहट से लगा कि धड़कनों की लय वापस सेट हो गई हो।
जोया पीछे खड़ी थी, एक पल के लिये चुप थी, फिर उसने दोनों को देख कर कहा, “कभी-कभी कहानी का सबसे जरूरी पन्ना वह होता है जो अंत में जुड़ा हो।” आदित्य ने जोया को देखा, मुस्कुरा कर कहा, “तुम्हारी कलम ने ये पन्ना लिखा है, और मैंने महसूस किया, कि मेरा नाम भी उस कविता में बैठता है।” उस शाम गंगा की लहरें दीपक बन कर जल रही थीं, उन अनंत पलों की तरह, जो छुए बिना भी जला जाते हैं। घाट पर आने वाले लोग चुप थे, जैसे उन्होंने भी समझ लिया हो कि यह दृश्य सिर्फ़ सपना नहीं, जीती हुई कविता है।
सावित्री ने अपनी डायरी खोली, और आख़िरी अधूरी पंक्ति लिखी — “यह जो लौट कर आया है, उसकी छाया में मैं फिर से खड़ी हूँ।” डायरी को लॉकर में फिर से रख दिया, क्योंकि अब यह वापसी का आख़िरी ठिकाना था। जोया ने आँसू पोंछते हुए कहा, “अब तुम वापस जा सकती हो,” और आदित्य ने माथे पर हाथ रख मंत्रमुग्ध होकर सूँघा — पहले गुलाब, फिर धूप, और फिर कविता की लय।
जोया ने दोनों के बीच आकर कहा, “मैं यह कहानी घर पर लिखूंगी, पर यह दीवारें, ये घाट, ये दोपहर की खिड़की — ये सब यहीं रहेंगे। मैं सबको दिखाऊँगी कि एक खिड़की कैसे दरवाज़ा बन सकती है।” सावित्री ने सिर हिलाया, उसकी बातें अब आदत नहीं, जीवन बन चुकी थीं।
अगली सुबह, तीनों ने घाट से विदा ली। जोया ने एक किताब खरीदी — ‘गंगा की कहानियाँ’ — जिसमें कहा गया था, “हर पल धारा बन कर बहता है, पर उसके किनारे कभी न सूखें।” वे तीनों अलग-अलग रेलगाड़ी पकड़ने गए — सावित्री दिल्ली, आदित्य बनारस, और जोया दिल्ली की पत्रिका के ऑफिस। पर जो दूरी थी, वह सिर्फ़ ज़मीनी थी; उनके रिश्ते अब नभ की सीमा को छू रहे थे।
रेल में बैठ कर सावित्री ने खिड़की से बाहर देखा। मोती जैसे हर खेत में झिलमिला रहे थे, पर उसकी आँखों में केवल एक खिड़की थी — उसकी दोपहर की खिड़की, जो अब किसी इमारत का हिस्सा नहीं, बल्कि हर उस दिल का हिस्सा बन चुकी थी जिसने अधूरी दास्तान सुनी और फिर खामोशी से पूरी की।
और उस पल उसने तय किया — चाहे हजार किताबें जन्म लें, चाहे न जाने कितनी लौटकर आने की चिट्ठियाँ आएँ, वह हमेशा वहीँ लौटेगी — अपनी दोपहर की खिड़की पर, जहाँ चाय की गर्माहट और धूप की मुस्कान हमेशा बाकी रहेगी।
****