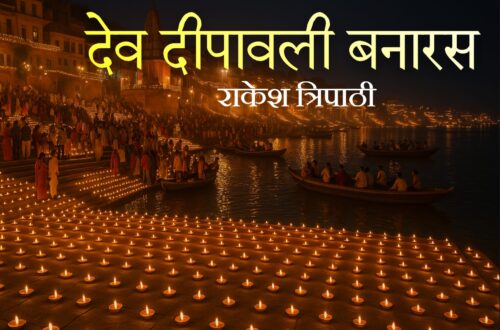अनामिका जोशी
1
शाम की हवा में अजीब सी उदासी थी, जैसे दिन अपने पैरों के निशान समेट रहा हो। दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर मयंक एक बेंच पर बैठा था, अपने नीले डफल बैग के ऊपर कोहनी टिकाए, और दूसरी ओर एक किताब पकड़े—”Norwegian Wood”। कानों में ईयरफोन, लेकिन कोई गाना नहीं चल रहा था। बस, शोर से खुद को काटने की एक कोशिश थी।
उसे ट्रेन पकड़नी थी—जयपुर जाने वाली इंटरसिटी। पहली नौकरी, पहली पोस्टिंग, और पहली बार दिल्ली छोड़ना। भीतर कुछ हल्का सा डर भी था और थोड़ा गर्व भी। आसपास लोग भागदौड़ कर रहे थे, किसी के हाथ में सैमसंग बैग, किसी के हाथ में रिश्तों की थकान। लेकिन मयंक शांत था। शांत और थोड़ा खोया हुआ।
“मुराकामी?” आवाज़ हल्की थी लेकिन साफ़। मयंक ने सिर उठाया।
उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। पिंक दुपट्टा, नीली जींस, और एक टोट बैग जिसमें एक बड़ा कॉफी मग झाँक रहा था। बाल खुले थे, चेहरे पर हल्की थकान और आँखों में एक तेज़ जिज्ञासा।
“हाँ,” मयंक ने जवाब दिया।
“थोड़ा उदास करता है न?” उसने पूछा, बगल में बैठते हुए।
मयंक हल्का मुस्काया, “अभी शुरुआत है। देखते हैं।”
लड़की ने हाथ बढ़ाया, “सिया। और तुम?”
“मयंक,” उसने हाथ मिलाया।
“कहाँ जा रहे हो?”
“जयपुर। नौकरी जॉइन करनी है।”
“वाह! मैं भी वही जा रही हूँ। मामाजी के पास। कुछ दिन ठहरने।”
मयंक को अजीब संयोग सा लगा। इतनी बड़ी दुनिया, और प्लेटफॉर्म पर दो अजनबी एक ही जगह जा रहे हैं।
“तुम क्या करती हो?” मयंक ने पूछा।
“मैं लिखती हूँ। कविताएँ, ब्लॉग, कभी-कभी किरदार भी।”
“किरदार?”
“हाँ,” सिया ने मुस्कराते हुए कहा, “जैसे अब तुम एक किरदार हो। मयंक—स्टेशन वाली मुलाक़ात।”
मयंक को पहली बार लगा, जैसे कोई उसे बिना पूछे ही समझ गया हो। उसे ये लड़की दिलचस्प लगी। बात करने वाली, देखने वाली नहीं—महसूस करने वाली।
ट्रेन आई। सीटी की आवाज़ और भीड़ की हड़बड़ी में भी सिया मयंक के साथ ही चढ़ी। उनकी सीटें आमने-सामने थीं। जैसे कहानी खुद आगे बढ़ रही थी।
ट्रेन चली। शहर पीछे छूटता गया और बातों का शहर उनके बीच बसता गया।
सिया ने मयंक से उसके कॉलेज, दोस्तों, फेवरेट मूवीज, और यहां तक कि उसकी बचपन की शरारतें भी पूछ लीं। और खुद के बारे में बताया कि कैसे उसने एक बार ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए एक कविता लिखी थी—जिसमें स्टेशन की चाय, प्लेटफॉर्म की आवाज़ें और जाते लोग सब एक अधूरे ख़त की तरह थे।
मयंक को वो सब सुनना अच्छा लगने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सफर जितना लंबा होगा, उतना ही उसकी यादों में गहराई से बस जाएगा।
“तुम्हें नहीं लगता कि ट्रेन की खिड़की से बाहर की दुनिया किसी दूसरी फिल्म जैसी होती है?” सिया ने पूछा।
“हां,” मयंक बोला, “और हम सिर्फ एक सीन में हैं।”
“पर क्या पता, वो सीन ही पूरी फिल्म बदल दे।”
रात हो गई थी। बाकी यात्री सो चुके थे। लेकिन उनकी बातचीत अब भी जारी थी। बाहर अंधेरा था, अंदर हल्की-सी लाइट और उनकी धीमी आवाज़ें।
“कभी-कभी लगता है न कि किसी अनजान को अपनी बात कहना आसान होता है?” सिया बोली।
“क्योंकि वो जज नहीं करता,” मयंक ने कहा।
“या शायद इसलिए कि हमें पता होता है कि वो चला जाएगा।”
कुछ देर खामोशी रही। फिर सिया ने पूछा, “अगर ये सफर कल खत्म हो जाए, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे?”
“नहीं,” मयंक ने सीधे उसकी आँखों में देखा, “क्योंकि कुछ लोग छूट कर भी रह जाते हैं।”
सुबह होने को थी। ट्रेन ने जयपुर का इशारा दिया।
दोनों चुप थे अब। जैसे कुछ कहने की ज़रूरत ही न रही हो।
स्टेशन आया, लोग उतरे, भीड़ तेज़ हो गई। सिया भीड़ में खो गई। मयंक ने इधर-उधर देखा, लेकिन वो नहीं दिखी।
वो बैग उठाकर निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज़ आई, “गुडबाय तो बोलोगे?”
सिया खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी।
“अगर कभी मिलना हो, तो सांगानेर की गलियों में ढूँढ़ लेना,” उसने कहा।
फिर वो चली गई।
और मयंक वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई कविता बिना अंतिम पंक्ति के रह गई हो।
2
जयपुर की हवा में वो मिठास थी जो पहली बार आने वालों को थोड़ा चौंकाती है और फिर बांध लेती है। मयंक का ऑफिस सिविल लाइंस में था, और उसकी पी.जी. सांगानेर के पास। पहला हफ़्ता व्यस्तताओं में बीता—नई जॉइनिंग, आई.डी. कार्ड, बैठकों की भीड़, और एक्सेल शीट्स के जंगल। लेकिन जैसे ही शाम आती, वो ट्रेन का सफर याद आ जाता। मयंक को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस वो चेहरे की हल्की मुस्कान, पिंक दुपट्टा और कहकहे जैसे उसकी आंखों में छप गए थे।
हर शाम ऑफिस से लौटते वक्त वो सांगानेर की तंग गलियों को यूँ ही भटकने लगता, जैसे उस एक वाक्य को ढूंढ रहा हो—”सांगानेर की गलियों में ढूंढ लेना।”
कितना बचकाना था ये—एक शहर में हज़ारों घर, हज़ारों चेहरे, और वो सोचता कि संयोग फिर साथ देगा? लेकिन कुछ बातें तर्क से नहीं, भाव से चलती हैं। और मयंक अब तर्क नहीं, तलाश में था।
एक दिन रविवार था। ऑफिस बंद। सूरज थोड़ा नरम, हवा में थोड़ी सर्दी। मयंक ने तय किया कि आज पूरी सांगानेर पैदल घूमेगा। मंदिर की घंटियाँ, हाथों में चूड़ियाँ पहनती महिलाएँ, साइकिल पर जाते दूधवाले—सब कुछ धीमा और फिल्मी सा लग रहा था।
और फिर एक मोड़ पर, उसने देखा—एक नीले दरवाज़े वाला घर, जिसकी छत पर कोई सूती चादरें फैला रहा था। उसके कानों में किसी की हँसी गूंज गई।
नीचे एक छोटा बोर्ड था: “काग़ज़ के फूल – कविता कार्यशाला, रविवार शाम 4 बजे”
उसका दिल धड़कने लगा। क्या यह वही है? क्या यह वही है जिसे वो ढूंढ रहा था?
वो ऊपर नहीं गया, बस दूर से देखा। थोड़ी देर तक छत की ओर नज़रें टिकाए रहा, फिर उल्टा मुड़ गया। डर था—अगर वो न निकली तो? या निकली, पर उसे याद न रहा हो?
शाम को चार बजे, वो फिर लौटा। इस बार धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ीं। ऊपर छत पर पांच-छह लोग बैठे थे—कागज़, कलम, और चाय की केतली के साथ। बीच में सिया थी। वही पिंक दुपट्टा, वही कॉफ़ी मग।
उसने मयंक को देखा, थोड़ी देर तक देखा। फिर हल्का सिर हिलाया। कोई चौंकाहट नहीं, कोई ‘तुम यहाँ?’ नहीं। जैसे वो जानती थी कि वो आएगा।
मयंक थोड़ी हिचक के साथ पास गया। “हाय,” उसने कहा।
“हाय,” सिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया।
“मैं… यूं ही घूमते-घूमते…”
“घूमते हुए वही लोग मिलते हैं जो कहीं खो गए होते हैं,” सिया बोली, और उसके बगल की खाली कुर्सी की ओर इशारा किया।
बैठक शुरू हुई। सबने अपनी-अपनी कविताएँ पढ़ीं—कोई बारिश पर, कोई अकेलेपन पर, कोई टूटे रिश्तों पर।
सिया की बारी आई तो उसने एक नई कविता पढ़ी, शीर्षक था—“अजनबी का स्टेशन”।
कविता में एक ट्रेन थी, एक किताब, नीला बैग, और अधूरी बातों वाली खिड़की। मयंक चुपचाप सुनता रहा। वो जान गया कि कविता उसी के लिए थी।
बैठक के बाद सब चले गए। सिर्फ सिया और मयंक बचे।
“तुम्हें सच में खोजा था?” उसने पूछा।
“मैंने तो तुम्हें रास्ता बता दिया था,” सिया ने कहा, “तुम चले आए।”
“क्यों?”
“क्योंकि कुछ मुलाक़ातें अधूरी नहीं छोड़ी जातीं।”
मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोस्ती? या उससे ज़्यादा?
“तुम हर रविवार यहाँ होती हो?”
“कभी-कभी। जब मन हो। जब कोई अधूरी कविता पूरी करनी हो।”
वो दोनों छत की मुंडेर पर खड़े हो गए। नीचे लाइटें जलने लगी थीं। दूर मंदिर से आरती की आवाज़ आ रही थी।
“क्या तुम मुझे जानने दोगी?” मयंक ने पूछा।
“अगर जानने का मतलब है साथ चलना, तो हाँ,” सिया बोली।
वो एक नई शुरुआत थी। बिना इजाज़त के नहीं, लेकिन बिना वादों के भी नहीं।
3
सिया और मयंक की मुलाकात अब एक आदत बन गई थी—बिना कहे, बिना तय किए। हर रविवार “कागज़ के फूल” की बैठक होती, जिसमें शहर के अलग-अलग छोर से कुछ शब्दप्रेमी इकट्ठा होते। लेकिन उन सबके बीच सिया और मयंक का संवाद कुछ और था—कभी चुपचाप बैठना, कभी आँखों से सवाल करना, कभी चाय के कप में हल्की सी हँसी घोलना।
उनकी बातचीतों में कभी “हम क्या हैं?” जैसी उलझी हुई जिज्ञासाएँ नहीं होती थीं। जैसे दो लोग बस एक ही ज़ुबान में सोचते थे—शब्दों की नहीं, मौन की।
एक रविवार, बैठक के बाद सिया बोली, “आज कहीं और चलते हैं, भीड़ से थोड़ा दूर।”
“कहाँ?” मयंक ने पूछा।
“मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ।”
ऑटो लिया गया। शहर पीछे छूटता गया और एक पुराना मोहल्ला सामने आया—खोया-सा, पुरानी हवेलियों और टूटी नामपट्टियों वाला।
एक खिड़की के नीचे सिया रुकी। वहां कुछ टूटे ख्वाबों की धूल थी, और कुछ यादों की परतें।
“यह मेरी नानी का घर था,” उसने कहा। “अब कोई नहीं रहता। बस मैं कभी-कभी आती हूँ, जब कुछ कहना होता है।”
मयंक ने देखा—उस खिड़की से रोशनी सी झाँक रही थी, जैसे भीतर कोई अब भी बैठा हो।
“तुम्हें लगा होगा मैं बहुत बोलती हूँ,” सिया बोली, “पर असल में मैं बहुत कुछ कह नहीं पाती।”
“जो चुप रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं,” मयंक ने कहा।
सिया मुस्कराई। “कभी-कभी लगता है कि तुम मेरे ही शब्दों को बोल रहे हो।”
वे उस पुराने घर की सीढ़ियों पर बैठ गए। आसपास कोई नहीं था। शहर की आवाज़ें दूर हो गई थीं।
“तुम्हारी कोई कहानी है?” सिया ने पूछा।
मयंक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, “एक अधूरी नौकरी के ख्वाब से भागा था, दूसरी पकड़ी है। घर में सबको लगता है मैंने ठीक किया, लेकिन मन अब भी वही पुरानी लाइब्रेरी ढूँढता है जहां मैं घंटों पढ़ा करता था।”
“और प्यार?” सिया ने सीधा सवाल पूछा।
“हुआ था,” मयंक बोला, “लेकिन खत्म नहीं हुआ—बस अलग हो गया।”
सिया ने आँखें झुका लीं। “मुझसे भी किसी ने एक बार कहा था कि ‘तुम बहुत जटिल हो’। मैंने जवाब में बस इतना कहा था कि ‘मैं पूरी हूँ, तुम छोटे पन्ने लेकर पढ़ रहे हो।’”
मयंक ने उसकी ओर देखा। कुछ टूटने की आवाज़ थी उस मुस्कान के पीछे, जैसे उसने किसी अपने को खोकर हँसना सीखा हो।
“क्या हम कुछ बन रहे हैं?” मयंक ने अचानक पूछा।
सिया चुप रही।
“मतलब, ये सब… जो है हमारे बीच… उसे कोई नाम चाहिए क्या?”
“नाम की ज़रूरत तब होती है जब खोने का डर हो,” सिया बोली। “और मुझे लगता है तुम वैसे नहीं हो जो खो दोगे।”
एक हल्की हवा चली। पत्तियाँ सरसराईं।
“तुम्हें देखता हूँ तो लगता है मैं अपने साथ बैठा हूँ,” मयंक ने कहा। “तुम्हारे साथ कोई भूमिका नहीं निभानी पड़ती।”
“कभी-कभी लोग मिलते हैं जो हमें हमारे ही भीतर वापस ले जाते हैं,” सिया बोली। “तुम ऐसे हो।”
वो खामोशी अब बोझिल नहीं थी। वो साथ थी। जैसे शब्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं रही।
रात होने लगी। उन्होंने उस पुराने घर को अलविदा कहा। जाते-जाते सिया ने एक पुरानी किताब उसे थमा दी।
“यह मेरी नानी की है। हर बार जब मैं खो जाती हूँ, इसे पढ़ती हूँ।”
मयंक ने किताब खोली—भीतर एक कविता थी, हाथ से लिखी हुई।
“अगर तुम कभी लौटो,
तो दरवाज़ा खटका देना मत—
मैं इंतज़ार में हूँ,
और ये खिड़की खुली है।”
मयंक ने किताब सीने से लगा ली।
सिया कुछ नहीं बोली, बस चल दी। और मयंक वहीं खड़ा रहा, जैसे पहली बार उसके पास कोई अधूरी चीज़ पूरी हो रही हो।
4
जयपुर की सर्दियाँ धीरे-धीरे उतर रही थीं। सड़कें धुंध से घिरी, खिड़कियों पर भाप की परत, और हाथों में गरम चाय की तलाश। ऐसे ही एक ठंडी सुबह, मयंक अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था जब दरवाजे के नीचे से एक छोटा-सा कागज़ सरकता दिखा।
उसे उठाकर देखा—कविता की एक पंक्ति थी।
“हर बार तुम्हें छोड़ देने की सोचता हूँ,
और हर बार तुम्हें अपने भीतर और गहरे पाता हूँ।”
नीचे नाम नहीं था, लेकिन उसे पहचानने में देर नहीं लगी—सिया।
पिछले एक महीने से उनके बीच की मुलाकातें एक लय में ढलने लगी थीं। कभी रविवार को कविता बैठक, कभी यूं ही बाजार में टकरा जाना, कभी एक-दूसरे को किताबें देना, और कभी बस चुपचाप साथ बैठ जाना।
मयंक अक्सर सोचता—क्या ये प्यार है? लेकिन फिर लगता, अगर है भी, तो क्या जरूरी है उसे किसी परिभाषा में बांधना?
उस दिन लंच ब्रेक में, उसने सिया को मैसेज किया—“आज शाम चाय?”
जवाब आया, “कहां?”
“जहां दो चाय, दो चुप्पियाँ और दो धड़कनों को कुछ कहने की ज़रूरत न हो।”
“तो फिर वही पुरानी किताबों वाली दुकान के सामने वाली टपरी?”
“बिलकुल।”
शाम को दोनों मिले। चाय की दुकान वैसी ही थी—बेंच थोड़ी टेढ़ी, चायवाले की आवाज़ थोड़ी ऊँची, लेकिन बीच में जो चुप्पी थी, वो सबसे साफ़ थी।
सिया आज पीले स्वेटर में थी, बाल बंधे हुए, लेकिन आंखें खुली किताब जैसी। मयंक ने आते ही दो चाय मंगाई।
“आजकल तुम्हारी कविताओं में उदासी कुछ ज़्यादा है,” उसने कहा।
“उदासी नहीं,” सिया बोली, “संवेदनशीलता है। जब दुनिया की चुभन महसूस होती है, तब ही तो असली कविता निकलती है।”
“या जब कोई भीतर का हिस्सा बार-बार तुम्हें किसी की याद दिलाता है।”
सिया ने एक लंबी सांस ली।
“तुमसे कुछ कहूँ?” उसने पूछा।
“तुम्हारा कहा न कहा, दोनों सुनता हूँ,” मयंक बोला।
“मुझे डर लगता है,” सिया ने धीमे से कहा।
“किस बात का?”
“कि हम ठीक हैं। बहुत ठीक। और मुझे आदत हो रही है—तुम्हारी, तुम्हारी खामोशी की, तुम्हारे देखने के तरीके की। और ये आदतें, सबसे ज़्यादा डराती हैं।”
“क्योंकि वो टूट सकती हैं?” मयंक ने पूछा।
सिया ने सर हिलाया।
“जब कोई बहुत करीब आता है, मैं खुद से दूर होने लगती हूँ। मुझे डर है कि मैं फिर से कहीं गुम न हो जाऊँ।”
मयंक ने उसकी ओर देखा। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन उसकी आवाज़ में तपिश थी।
“अगर तुम कभी गुम हो भी गई,” मयंक बोला, “तो मैं वही रहूँगा जहां तुमने मुझे छोड़ा था।”
सिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कराई। “तुम्हें नहीं लगता कि हम किसी पुराने जन्म के अधूरे संवाद को जी रहे हैं?”
“या शायद इस जन्म के किसी बहुत धीमे प्रेम को,” मयंक बोला।
चाय खत्म हुई। आसमान में हल्का सा कुहासा उतर आया था। दुकान के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन में अकेलापन था, लेकिन कोई शिकायत नहीं।
सिया ने पूछा, “क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी एक होंगे?”
मयंक ने जवाब नहीं दिया। बस उसकी ओर देखा, जैसे उसका होना ही सबसे सच्चा जवाब हो।
“मेरे लिए यह रिश्ता वैसे है जैसे अधूरी कविता,” सिया बोली, “हर बार सोचा खत्म कर दूँ, लेकिन हर बार एक नई लाइन जुड़ जाती है।”
“तो क्यों न उसे पूरा होने दें?” मयंक ने पूछा।
“क्योंकि शायद कुछ कविताएँ अधूरी ही सबसे सुंदर होती हैं,” सिया ने धीमे से कहा।
उस रात दोनों अपने-अपने घर लौटे, लेकिन भीतर एक अजीब सा सुकून और बेचैनी साथ आई। जैसे दिल ने एक-दूसरे को महसूस करना शुरू कर दिया हो—बिना कहे, बिना छुए।
मयंक ने उस रात अपनी डायरी में लिखा:
“तुमसे मिलना, जैसे किसी पुराने ख्वाब का दरवाज़ा खुलना।
तुमसे बात करना, जैसे खामोशी का कोई नया अर्थ गढ़ना।
तुम्हारे बिना भी तुमसे जुड़ा हूँ—क्योंकि तुम अब मेरे अंदर हो,
बिलकुल मेरी लिखी हुई किसी कविता की तरह।”
5
जयपुर की सर्दियाँ अब अपना रंग जमा चुकी थीं। सुबह-सुबह की धूप भी खिड़कियों से झांकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मयंक को अब यह शहर अजनबी नहीं लगता था। ऑफिस, कैफे, वो पुरानी किताबों वाली दुकान, और सबसे बढ़कर—सिया।
हर रोज़ उनकी मुलाकात ज़रूरी नहीं थी, लेकिन हर रोज़ उनकी मौजूदगी एक-दूसरे में होती थी। किसी किताब की एक लाइन, किसी पुराने गाने की धुन, या किसी कैफ़े की खिड़की पर गिरे ओस की बूँदों में—सिया अब मयंक की दुनिया में हर जगह थी।
और अब सिया के लिए भी मयंक कोई कविता का किरदार नहीं, बल्कि उसकी ही कहानी का हिस्सा बनता जा रहा था।
फिर एक दिन कुछ बदल गया।
वो रविवार नहीं था, न ही “काग़ज़ के फूल” की बैठक थी। मयंक ऑफिस से लौट रहा था जब उसे सिया का मैसेज आया—”क्या मिल सकते हो अभी?”
बस इतना ही। न कोई स्माइली, न कोई इमोजी।
मयंक ने बिना सोचे टैक्सी ली और उस पुराने घर की ओर निकल पड़ा जहां पहली बार सिया ने उसे अपने भीतर झाँकने दिया था। दरवाज़ा आधा खुला था।
सिया अंदर बैठी थी—पीले लैंप की हल्की रौशनी में, एक पुरानी डायरी गोद में रखे, और आँखों में भारीपन।
“क्या हुआ?” मयंक ने धीरे से पूछा।
सिया ने उसकी ओर देखा, और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान अधूरी रह गई।
“मयंक… मेरी मम्मी आई हैं,” वो बोली।
“अचानक?”
“हाँ। और वो चाहती हैं मैं वापस चलूं। दिल्ली। अगले हफ़्ते।”
मयंक का दिल जैसे एक पल को रुक गया।
“पर क्यों?” उसने खुद को संयत रखते हुए पूछा।
“कुछ पारिवारिक चीज़ें हैं। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और मम्मी को लगता है अब वक्त है कि मैं अपनी ज़िंदगी ‘सीरियसली’ लूँ।”
“और तुम्हारे लिए… ये क्या है? हमारे लिए?”
सिया ने उसकी आँखों में देखा।
“यही तो उलझन है,” उसने कहा, “तुम हो, मयंक। और तुम्हारे साथ जो है, वो इतना गहरा, इतना सहज… लेकिन मेरे पास कोई वादा नहीं है, कोई दावा नहीं है कि मैं कल भी यहीं रहूँगी।”
मयंक ने कुछ नहीं कहा। बस धीरे-धीरे उसके पास बैठ गया। उनके बीच फिर से वही पुरानी चुप्पी आ गई—जो कभी सुकून देती थी, आज बोझ सी लग रही थी।
“क्या तुम चाहोगे कि मैं रुक जाऊँ?” सिया ने पूछा।
मयंक ने उसकी ओर देखा, बहुत ध्यान से।
“मैं चाहूँगा कि तुम वही करो जो तुम्हारे दिल को हल्का करे। अगर मेरे साथ रहना तुम्हारे भीतर डर भरता है, तो मत रहो। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए वो कोना हूँ जहाँ तुम खुद को सच्चा पाती हो, तो मत जाओ।”
सिया की आँखें नम हो गईं।
“तुमने हमेशा मुझे बिना मांगे समझा है,” वह बोली। “और शायद इसलिए मुझे डर लगता है—कहीं मैं तुम्हें वो सब न दे सकूं, जिसकी तुम हक़दार हो।”
“मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिया,” मयंक बोला, “तुम जैसी हो, वैसी। अधूरी, उलझी, खूबसूरत।”
कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर सिया ने अपनी डायरी मयंक की तरफ बढ़ा दी।
“यह मेरी नानी की डायरी है। उसमें कुछ अधूरी कविताएँ हैं। मैं चाहती थी कि तुम उन्हें पूरा करो। शायद तुम्हारे शब्दों में मेरी विरासत को नई आवाज़ मिले।”
मयंक ने डायरी ली जैसे कोई पवित्र चीज़ हो।
“तो क्या मैं समझूं… तुम जा रही हो?”
सिया ने सिर झुका लिया।
“शायद कुछ दिन के लिए… शायद हमेशा के लिए… मुझे नहीं पता।”
फिर उसने धीरे से कहा, “अगर ये सपना है, मयंक, तो प्रार्थना करना कि टूटे नहीं।”
उस रात मयंक देर तक जागता रहा। डायरी के पन्नों को पलटता रहा। हर पंक्ति में सिया की छवि दिखती रही।
> “खिड़की से गिरती धूप,
तेरी मुस्कान जैसी लगती है।
और जब बादल छा जाते हैं,
तो तुझसे बिछड़ने जैसा लगता है।”
वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। इंतज़ार सिर्फ तब तक सुंदर होता है, जब वो उम्मीद से बंधा हो।
अगले दिन सुबह-सुबह, मयंक ने एक सफेद लिफ़ाफ़ा तैयार किया। उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी और वो पन्ना जो उसने रात को लिखा था।
“तुम्हारे बिना भी तुमसे जुड़ा हूँ।
अगर जाना ही है, तो ले चलो मुझे भी।
या कम से कम बता दो—तुम किस मोड़ पर मिलोगी अगली बार।”
6
जयपुर की हवाओं में उस दिन कुछ भारीपन था। जैसे बादल खुद भी तय नहीं कर पा रहे थे कि बरसें या नहीं। और सिया की विदाई अब केवल एक भावना नहीं, एक तयशुदा समय हो चुकी थी। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी—दिल्ली के लिए।
मयंक ने रात भर नींद नहीं ली। उसकी खिड़की के बाहर जो गुलमोहर का पेड़ था, वो अब उसे वहीं से देखता लगा जहां पहली बार उसने सिया की कविताओं को समझना शुरू किया था। सबकुछ वैसा ही था, बस एक खालीपन पसरने लगा था—धीमा, लेकिन गहरा।
सुबह-सुबह मयंक स्टेशन पहुंचा। सिया ने नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी वो आया। कई बार बिन बुलाए आना ही सबसे सच्चा आना होता है।
प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर खड़ी ट्रेन की खिड़कियों से धुआँ और कोहरा आपस में घुलमिल गए थे। सिया नीले सूट में थी, वही पुराना पिंक दुपट्टा उसकी गर्दन से लहराता हुआ। उसके पास दो बैग थे—एक हाथ में, एक मन में।
मयंक थोड़ी दूरी से उसे देखता रहा। कुछ पल बीते। फिर सिया ने उसकी ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई घबराहट नहीं। बस वही शांति जो मयंक उसकी आंखों में हर बार पढ़ता था।
वो उसके पास आया।
“आखिरी बार पूछ सकता हूँ?” मयंक ने कहा।
“क्या?” सिया ने हल्के से पूछा।
“रुकोगी क्या?”
सिया चुप रही। एक सेकंड, दो सेकंड, और फिर बोली—“मयंक, कभी-कभी कुछ जगहों से निकलना इसलिए जरूरी होता है, ताकि हमें यह एहसास हो सके कि हम क्या खोना नहीं चाहते थे।”
“और जब तक वो एहसास होता है, क्या हम एक-दूसरे से छूट चुके होते हैं?”
“शायद नहीं। शायद हम और करीब हो चुके होते हैं। बस किसी और रूप में।”
मयंक ने जेब से वो सफेद लिफ़ाफ़ा निकाला।
“ये कल रात तुम्हारे लिए लिखा था,” उसने कहा।
सिया ने लिया नहीं, बस देखा।
“पढ़ोगी?”
“जरूर,” उसने मुस्कराते हुए कहा, “लेकिन ट्रेन में, अकेले में, जब मेरे पास खुद से मिलने का समय होगा।”
उसके बाद दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ट्रेन की सीटी बजी। कुछ पल बाकी थे।
“क्या तुम्हें डर नहीं लगता?” मयंक ने पूछा।
“बहुत,” सिया बोली। “पर डर से बड़ा ये यकीन है कि जो दिल से जुड़ता है, वो शहरों से नहीं टूटता।”
ट्रेन के दरवाज़े पर खड़े-खड़े सिया ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा।
“तुम वही रहना, मयंक,” उसने कहा, “जैसे तुम हो। मत बदलना, मत रुकना। मैं अगर लौटी… तो तुम्हें वैसा ही पाना चाहती हूँ।”
“और अगर नहीं लौटी?”
“तो तुम समझना कि मैं वहीं हूँ—जहाँ पहली बार हमारी बात अधूरी रह गई थी।”
ट्रेन चली गई।
मयंक वहीं खड़ा रह गया। शोर धीरे-धीरे दूर होता गया। लोग अपनी-अपनी मंज़िल की ओर चले गए। लेकिन उसकी मंज़िल… वही प्लेटफॉर्म पर छूट गई थी।
दिन बीतते गए। सिया नहीं लौटी।
लेकिन लौट आई उसकी कविताएँ।
हर हफ्ते मयंक को एक नीले लिफ़ाफ़े में एक चिट्ठी मिलती—दिल्ली से। हर चिट्ठी में एक कविता, एक स्मृति, और एक नया सवाल होता।
“क्या तुमने आज गुलमोहर को देखा?
उसने मेरी यादों को झटका तो नहीं दिया?”
“क्या तुम्हारे कमरे की खिड़की अब भी खुलती है सुबह-सुबह?
या तुमने भी उसे बंद करना सीख लिया?”
मयंक हर चिट्ठी को पढ़कर जवाब नहीं देता था। लेकिन वो लिखता ज़रूर था। डायरी में। अपनी नोटबुक में। और अपने ख़्वाबों में।
सिया उसके लिए अब कोई नाम नहीं थी। वो उसकी सोच थी, उसकी रूह में बसी कोई धड़कन जो शब्दों से नहीं, खामोशी से बजती थी।
एक दिन शाम को, ऑफिस से लौटते समय, मयंक वही पुरानी टपरी पर रुका जहां वे चाय पीते थे। चायवाले ने देखा और मुस्कराया, “आज अकेले?”
मयंक मुस्कराया, “नहीं, आदत के साथ हूँ।”
तभी उसकी निगाह सामने पड़ी—वहीं पुरानी बेंच, और उस पर रखा एक पिंक दुपट्टा।
दिल एक पल को रुक गया।
वो तेज़ी से उधर गया। दुपट्टा अब भी गरम था। जैसे किसी ने अभी ही छोड़ा हो।
उसने बेंच के नीचे झाँका। एक छोटी-सी किताब थी—उस पर लिखा था:
“तुम्हारे बिना भी तुमसे।”
नीचे नाम नहीं था।
बस एक पन्ना खुला हुआ था:
“जब तुमने जाना चाहा,
मैं वही थी—जहाँ तुमने छोड़ा था।
अब जब तुमने रुकना चाहा,
मैं वही हूँ—जहाँ से फिर मिल सकते हैं।”
मयंक ने किताब उठाई, आँखें बंद कीं, और मुस्कराया।
शायद ये इत्तेफ़ाक नहीं था।
शायद कुछ फासले सिर्फ मिलने के लिए ही आते हैं।
7
पिंक दुपट्टे की मुलायम गरमाहट उस बेंच पर अब भी थी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। और मयंक, जो कई हफ्तों से सिर्फ सिया की यादों के साथ जी रहा था, अचानक खुद को फिर उसी मोड़ पर पा रहा था जहां से सब शुरू हुआ था—एक चुप्पी, एक अधूरी बात, और एक उम्मीद।
उसने धीरे से किताब उठाई, “तुम्हारे बिना भी तुमसे।” पन्ने पुराने नहीं थे, लेकिन उनमें जो लिखा था, वो जैसे वक्त से बाहर था।
“अगर कभी लौट आऊँ,
तो सवाल मत पूछना—
बस देखना,
क्या मेरी आंखों में अब भी वही कविता है।”
मयंक ने उस पन्ने को हाथ में लिया, और फिर टपरी वाले से पूछा, “ये किसने छोड़ा?”
चायवाले ने कहा, “एक लड़की आई थी। बोली—‘अगर वो आए, तो कहना मैंने कुछ नहीं कहा।’ मुस्कराई और चली गई। तुम हो क्या वो?”
मयंक हँस पड़ा। “शायद हूँ।”
उसने उसी वक्त एक ऑटो लिया और उस पुराने हवेली जैसे घर की ओर निकल पड़ा जहाँ सिया ने उसे पहली बार नानी की कविताओं से मिलवाया था। घर अब भी वैसा ही था—दरवाज़ा आधा खुला, खिड़की से हल्की धूप अंदर आती हुई।
मयंक ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर कोई नहीं था, बस टेबल पर एक कॉफ़ी मग रखा था, और बगल में एक छोटा नोट:
“शब्द कभी ग़ायब नहीं होते।
वे बस इंतज़ार करते हैं सही पाठक का।
मैं यहीं थी। मैं यहीं हूँ।”
उसकी आँखों में नमी आ गई। इतनी नज़दीकी, इतनी चुपचाप? क्या सिया सच में लौटी थी?
उसी शाम, वो गया “कागज़ के फूल” की रविवार वाली बैठक में। सिया वहाँ नहीं थी। लेकिन एक नई लड़की आई थी—नाम था अन्वी, दिल्ली से आई थी। बोली, “सिया दी मेरी बड़ी बहन की दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा था जयपुर आकर इस ग्रुप में शामिल होने।”
मयंक चौक गया। “क्या उन्होंने कुछ भेजा है?”
अन्वी ने बैग से एक छोटा-सा लिफ़ाफ़ा निकाला।
मयंक ने उसे खोला।
“प्रिय मयंक,
कभी-कभी हमें अपने ही लिखे पन्नों को दूसरों के हाथों में सौंपना पड़ता है—ताकि हम समझ सकें कि वो कितने बहुमूल्य थे।
मैं तुम्हारे पास थी, हर उस शब्द में जो तुमने बिना बोले कहा। मैं अब लौट आई हूँ, लेकिन एक शर्त पर—अगर तुम चाहो तो।
कल शाम 5 बजे, वही किताबों वाली दुकान।
अगर आ सको, तो आना।
अगर न आ सको, तो समझूंगी—हमारी कहानी अब किताब बन चुकी है।”
अगले दिन, शाम पांच बजे।
मयंक वक्त से पहले पहुँचा। किताबों की दुकान पर हल्की-सी भीड़ थी। वो वहीं बैठ गया जहां सिया अक्सर कॉफ़ी मग के साथ किताबें पलटा करती थी। उसके सामने एक किताब पहले से रखी थी—“The Little Prince”—जिसके भीतर एक और चिट्ठी थी।
“तुम्हारे बिना भी तुमसे
जुड़ा रहना आसान नहीं था।
पर तुम्हारे साथ होकर
खुद से जुड़ना और भी मुश्किल हो जाता था।
क्या हम एक बार फिर मिल सकते हैं—
बिना वादे के, बिना डर के,
सिर्फ साथ होने के लिए?”
मयंक ने सिर उठाया।
सामने से सिया चली आ रही थी—धीमे कदम, वही पिंक दुपट्टा, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई उलझन नहीं थी।
दोनों एक-दूसरे के सामने रुके। किसी ने कुछ नहीं कहा।
फिर मयंक ने धीरे से पूछा, “ये सब… अचानक कैसे?”
“अचानक नहीं,” सिया बोली, “बस देर से हुआ। कुछ चीज़ें लौटती हैं—जब तुम उन्हें खो चुके मानते हो। मैं खुद से लौट आई हूँ।”
“और मैं अब भी वहीं हूँ,” मयंक बोला, “जहाँ तुमने छोड़ा था।”
“तो फिर?” सिया ने मुस्कुराकर पूछा।
“तो फिर हम वहीं से शुरू करें जहां पहली बार हमारी चुप्पियाँ मिली थीं।”
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
सिया ने पकड़ लिया।
अब न कोई वादा था, न परिभाषा। सिर्फ दो लोग थे—जिन्होंने एक-दूसरे को उस वक्त अपनाया था, जब कोई स्पष्टता नहीं थी।
और शायद यही सबसे सुंदर रिश्ते होते हैं—जहाँ दो अधूरी कविताएँ मिलकर एक पूरी किताब बनती हैं।
8
जयपुर की गलियाँ अब भी वैसी ही थीं—कभी शांत, कभी शोर से भरी, कभी धूप में भीगी, कभी भावनाओं से। फर्क बस इतना था कि इस बार मयंक और सिया साथ थे। कोई नाम नहीं था उनके रिश्ते का, लेकिन उनकी आँखों में अब परिभाषाओं की ज़रूरत भी नहीं थी।
कभी-कभी सिया मयंक के ऑफिस के पास वाले कैफे में बैठती, कॉफ़ी का मग थामे अपनी नोटबुक में कुछ लिखती रहती। और मयंक, मीटिंग्स के बीच जब खिड़की से झाँकता, तो उसे देखकर खुद को हल्का महसूस करता। जैसे सबकुछ उलझा हुआ होते हुए भी, उसके जीवन में एक कोना ऐसा है जो पूरी तरह सुलझा है।
एक दिन, सिया बोली, “हमारा क्या चल रहा है मयंक?”
मयंक हँसा, “अभी भी वही सवाल?”
“नहीं, अब थोड़ा अलग। अब मैं ये नहीं पूछ रही कि हम क्या हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि हम चल किस ओर रहे हैं?”
मयंक थोड़ी देर चुप रहा।
“शायद हम किसी ओर नहीं चल रहे, सिया,” उसने कहा, “शायद हम वहीं ठहरे हुए हैं, जहाँ एक कविता बस लिखी जा रही है—धीरे-धीरे, हर रोज़।”
“और अगर किसी दिन कविता पूरी हो जाए?”
“तो हम नई कविता शुरू करेंगे,” मयंक ने मुस्कुराकर कहा।
सिया ने सिर झुका लिया।
“लेकिन एक डर है मयंक… जो अब भी साथ चलता है। डर कि ये सब कोई सपना न हो। कि एक दिन ये सुबहें, ये शामें, ये बातें… सब छूट न जाएँ।”
“अगर छूट जाएँ,” मयंक बोला, “तो भी वो हमारे भीतर ज़िंदा रहेंगी। यादों की तरह, या आदतों की तरह। पर जब तक हैं, तब तक पूरी तरह जिएँ उन्हें। चलो हर दिन को आखिरी जैसा जीते हैं।”
इस बात के कुछ हफ़्ते बाद, एक ऑफ़िस इवेंट के सिलसिले में मयंक को मुंबई जाना पड़ा—एक हफ्ते के लिए। उसने सिया को कहा, “आउंगा, तो समुद्र की कहानी सुनाऊँगा।”
सिया मुस्कुराई, “और मैं हवाओं की कविता लिख कर रखूँगी।”
विदाई के वक्त दोनों एक-दूसरे को देख रहे थे—भीड़ के बीच दो लोग, जिनके पास एक ही भाषा थी: मौन।
मुंबई में मयंक का हफ्ता व्यस्त रहा। मीटिंग्स, होटल, ट्रैफ़िक, और समुद्र की नमी। लेकिन हर शाम जब वो अपने होटल की बालकनी में बैठता, उसकी आँखों के सामने सिया का चेहरा होता। उसके हाथ अनायास ही उसकी नोटबुक पर चलने लगते—हर पंक्ति, हर शब्द, सिया की यादों से लिपटा हुआ।
“तुम अगर होतीं,
तो ये लहरें भी धीमी चलतीं।
और समंदर… शायद खुद को थोड़ा छोटा कर लेता।”
इधर जयपुर में सिया भी रोज़ उसे याद करती रही। उसकी कविताओं में अब थोड़ी बेचैनी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि मयंक की मौजूदगी उसे सिर्फ सुकून नहीं, हिम्मत भी देती थी।
एक शाम उसने डायरी में लिखा:
“तुम नहीं हो,
फिर भी हो।
तुम्हारे बिना भी,
मैं तुमसे लिख रही हूँ।”
मयंक की वापसी वाले दिन, सिया स्टेशन पर नहीं आई।
वो हैरान था। थोड़ा परेशान भी।
ऑटो लेकर वो सीधे उस पुराने घर की ओर गया, जहाँ हमेशा सिया मिलती थी—दरवाज़े के पीछे, या खिड़की के पार।
लेकिन घर बंद था। ताला लगा हुआ।
कोई नोट नहीं, कोई संदेश नहीं।
उस रात मयंक को नींद नहीं आई।
क्या हुआ? क्या फिर से वो चली गई?
अगली सुबह, उसकी ऑफिस डेस्क पर एक छोटा पार्सल रखा था।
खोलते ही अंदर एक किताब मिली—उसकी खुद की लिखी पंक्तियाँ, जिनमें सिया ने नई पंक्तियाँ जोड़ दी थीं।
हर दो पंक्तियों के बाद, उसकी एक नई कविता।
आखिरी पन्ने पर लिखा था:
“मैं यहाँ हूँ। बस थोड़ा अपने भीतर चली गई थी।
तुमसे जुड़कर, मैं खुद से मिल रही हूँ।
और अब जब लौटूँगी,
तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं—हमारे लिए।”
मयंक ने किताब सीने से लगा ली।
उसे अब भी सिया नहीं मिली थी, लेकिन वो जानता था—कुछ रिश्ते हर मोड़ पर मिलने का रास्ता बना लेते हैं। उनके पास मंज़िल नहीं होती, लेकिन साथ होता है।
और यही साथ, सबसे बड़ा घर बन जाता है।
9
जयपुर की सुबहें पहले से कुछ बदल गई थीं। मयंक की बालकनी में रखे तुलसी के पौधे पर ओस की बूँदें अब भी पड़ती थीं, लेकिन उनमें वो चमक नहीं थी जो सिया के साथ के दिनों में थी। किताबों वाली दुकान अब भी खुलती थी, लेकिन मयंक वहाँ बस किताबें नहीं, यादें पलटने जाता था।
सिया की भेजी किताब अब उसकी सबसे कीमती चीज़ बन चुकी थी। हर बार जब उसे कुछ समझ नहीं आता, जब कोई बात दिल को बेचैन करती, वो उस किताब का एक पन्ना खोलता और सिया की लिखी कोई पंक्ति पढ़ लेता:
“तुम्हारी खामोशी में भी
मैं अपनी पुकार सुन लेती हूँ।”
पर वो कब लौटेगी? क्या लौटेगी? या फिर ये सारी बातचीत अब सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह जाएगी?
मयंक को नहीं पता था, लेकिन वो यक़ीन करता रहा।
एक दिन ऑफिस से लौटते समय, मयंक को एक मैसेज मिला—“छत पर आओ।”
कोई नाम नहीं था। कोई इमोजी भी नहीं। लेकिन मयंक को पता था ये किसका हो सकता है।
वो अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ता गया—धीरे, लेकिन धड़कनों के शोर के साथ। जैसे हर कदम किसी पुराने सपने के करीब ले जा रहा हो।
छत पर हल्का अंधेरा था। चाँद पूरा नहीं था, लेकिन रौशनी काफी थी।
और वहाँ… सिया खड़ी थी।
वही पिंक दुपट्टा, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आँखों में स्थिरता थी।
“तुम?” मयंक की आवाज़ जैसे गले में अटक गई।
“मैं,” सिया ने कहा, “अब पूरी तरह से।”
दोनों कुछ पल तक सिर्फ देखते रहे। कुछ भी कहे बिना।
“मैं डर गई थी,” सिया बोली, “कि मैं जो चाहती हूँ, शायद वो तुमसे ज़्यादा माँग लेगी। इसलिए मैंने खुद से दूरी बना ली… ये समझने के लिए कि क्या वाकई मैं तुम्हारे साथ की ज़रूरत महसूस करती हूँ… या बस आदत थी।”
“और?” मयंक ने धीमे से पूछा।
“और मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे भीतर किसी आदत की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरत की तरह बस चुके हो। जैसे साँस। जैसे कविता।”
“फिर क्यों चली गई थीं?”
“ताकि जब लौटूँ, तो तुम्हारे पास पूरी रह सकूँ। बिना शक, बिना डर, बिना अधूरेपन के।”
मयंक ने एक लंबी सांस ली।
“तुम्हारे बिना दिन कटते थे,” उसने कहा, “लेकिन पूरे नहीं होते थे।”
सिया पास आई। “अब जब मैं हूँ, तो क्या तुम मुझे थामोगे? जैसे शब्द काग़ज़ को थामते हैं? कोई परिभाषा नहीं चाहिए मुझे। कोई वादा भी नहीं। सिर्फ साथ… वो जो हमारी खामोशियों में है।”
“मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं माँगा,” मयंक बोला। “लेकिन अगर तुम मेरी हो, तो मेरी दुनिया फिर से कविता बन जाएगी।”
सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया।
उनकी हथेलियों के बीच कोई कसमें नहीं थीं। बस स्पर्श था—गहरा, सच्चा, और शांत।
अगले कुछ हफ्ते जैसे किसी दूसरी दुनिया में बीते। अब सिया और मयंक के बीच संवाद और भी खामोश हो गया था—क्योंकि अब शब्दों की ज़रूरत कम पड़ने लगी थी।
एक शाम दोनों शहर से दूर एक पुराने बाग़ में गए। वहाँ सिया ने एक टिफ़िन निकाला, जिसमें दो कप चाय और कुछ बिस्किट थे।
“याद है?” सिया मुस्कराई।
“ट्रेन वाला सफर?” मयंक हँसा, “तुमने उस दिन मुझे बिस्किट खिलाया था।”
“और तुमने मुराकामी पढ़ना छोड़ा था,” सिया बोली।
“अब मैं तुम्हें पढ़ता हूँ,” मयंक ने कहा।
“तो फिर बताओ, मेरी सबसे पसंदीदा लाइन कौन-सी है?”
मयंक ने ज़रा भी सोचे बिना कहा—
“कभी-कभी, सबसे अच्छा साथी वो होता है जो कुछ नहीं कहता, बस मौजूद रहता है।”
सिया की आँखें भर आईं।
“मुझे डर था, मयंक, कि लौटने के बाद सब बदल जाएगा। लेकिन तुम अब भी वही हो… और अब मैं भी वही हूँ, जो रहना चाहती थी।”
“हम अब भी वो नहीं हैं जो दुनिया परिभाषित करे,” मयंक बोला, “लेकिन हम हैं… पूरे, साथ, और सच्चे।”
सिया ने उसे देखा।
“क्या हमारी कहानी यहीं पूरी हो जाती है?” उसने पूछा।
मयंक ने मुस्कराकर सिर हिलाया।
“नहीं,” वह बोला, “यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है—बिना ब्रेक के, बिना एडिटिंग के, एक लय में बहती हुई। जैसे तुम और मैं, साथ।”
उसी रात, सिया ने अपनी डायरी में लिखा:
“मैं लौट आई हूँ।
न किसी मजबूरी से,
न किसी मोह से।
बस इसलिए कि मेरा घर वहीं है
जहाँ तुम हो।”
10
सर्दी अब ढलने लगी थी। गुलमोहर के पेड़ फिर से कोंपलों से भरने लगे थे, और हवा में हल्की सी गर्माहट घुलने लगी थी। जयपुर की इस शांत संध्या में, मयंक और सिया पुराने घर की छत पर बैठे थे—जहाँ से शहर आधा दिखता था और आधा छुपा रहता था।
दोनों चुप थे, लेकिन इस बार उनकी चुप्पी में कोई उलझन नहीं थी। अब वे शब्दों से नहीं, उपस्थिति से जुड़े हुए थे।
“जानते हो,” सिया ने कहा, “कभी-कभी सोचती हूँ, अगर हम पहली बार ट्रेन में न मिलते तो?”
“तो शायद कहीं और मिलते,” मयंक ने जवाब दिया। “किसी किताब के कोने में, या किसी कविता की लकीर में। क्योंकि मुझे अब लगता है, तुम्हारा मिलना तय था। बस तरीका अलग हो सकता था।”
सिया मुस्कुरा दी।
“और तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़े पुराने ज़माने के लोग हैं?”
“मतलब?”
“मतलब… अब लोग रिश्तों में इंस्टैंट कॉफी की तरह फैसले लेते हैं। फॉलो, डेट, ब्रेकअप, ब्लॉक। और हम… दो चाय, बीस चुप्पियाँ, और महीनों की दूरी के बाद भी बस एक साथ बैठने का सुकून।”
“तो क्या तुम्हें लगता है हम असामान्य हैं?” मयंक ने पूछा।
“शायद नहीं,” सिया बोली, “शायद हम बस उन लोगों में हैं जो कहानी को जीने में यकीन रखते हैं, सुनाने में नहीं।”
छत की रेलिंग पर बैठे कबूतर उड़े। और उस उड़ान के साथ कुछ बीती बातें भी उड़ गईं—डर, भ्रम, बेचैनियाँ।
अब जो बचा था, वो था बस ‘आज’। और आज बहुत सुंदर था।
अगले हफ्ते “कागज़ के फूल” की बैठक थी। इस बार सिया और मयंक दोनों एक साथ पहुँचे। नए लोग थे, कुछ पुराने चेहरे भी।
सिया ने कहा, “आज हम मिलकर एक कविता पढ़ेंगे।”
फिर उसने डायरी खोली, और मयंक के साथ मिलकर पढ़ना शुरू किया—एक-एक पंक्ति, एक-एक साँस के साथ।
“वो मुलाक़ात थी, शायद संयोग से,
स्टेशन की भीड़ में जब एक कहानी शुरू हुई।
बिस्किट और मुराकामी के बीच,
कोई खिड़की थी, जहाँ से ज़िंदगी झाँक रही थी।
फिर फासले आए, चिट्ठियाँ बनीं,
कुछ अधूरी कविताएँ पूरी हुईं।
और आज जब तुम पास बैठे हो,
तो लगता है, शब्द खुद को पढ़ रहे हैं।”
बैठक के अंत में तालियाँ नहीं बजीं। बस एक गहरी, लंबी खामोशी थी—सम्मान की, समझ की, और शायद इस बात की कि हर किसी को ऐसा कोई नहीं मिलता, जो तुम्हारी खामोशी को कविता बना दे।
उस रात, सिया और मयंक साथ में चाय पी रहे थे।
“तुम्हें पता है,” सिया बोली, “हमने कभी ‘आई लव यू’ नहीं कहा।”
“हाँ,” मयंक मुस्कराया, “क्योंकि हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे हर लौटने में, और मेरे हर इंतज़ार में, वो बात पहले ही छिपी थी।”
सिया ने हाथ आगे बढ़ाया, “फिर भी, आज मैं कहना चाहती हूँ।”
“क्या?” मयंक ने धीमे से पूछा।
“मैं तुमसे प्यार करती हूँ,” सिया बोली।
मयंक ने उसकी आँखों में देखा, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया।
“और मैं तुम्हें। शायद हमेशा से। बस आज, शब्द मिल गए हैं।”
समय बीता, लेकिन उनकी दुनिया वैसी ही रही—कविताओं में बसी, कहानियों में लिपटी, और एक-दूसरे की सांसों में धड़कती।
कभी सिया जयपुर के किसी छोटे स्कूल में बच्चों को कविता सिखाती, तो मयंक अपनी रिपोर्ट्स के बीच उसका लिखा कोई नया पन्ना पढ़ लेता।
उन्होंने कभी शादी नहीं की—कम से कम उस अर्थ में नहीं, जैसा समाज सोचता है। उनके पास सिंदूर नहीं था, न ही फेरे। लेकिन जो था, वो कहीं ज़्यादा स्थायी था।
एक दिन सिया ने अपनी नई डायरी मयंक को दी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था—
“तुम्हारे बिना भी तुमसे जुड़ी रही।
अब जब तुम साथ हो,
तो मैं खुद से भी जुड़ गई हूँ।
ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती।
ये कहानी… अब तुम्हारे पास रहती है।”
अंतिम पंक्तियाँ —
कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं, लोगों में बसती हैं।
कुछ रिश्ते वादों से नहीं, मौन से जुड़े होते हैं।
और कुछ प्रेम…
कुछ प्रेम वो होते हैं जो ‘तुम्हारे बिना भी’
सिर्फ ‘तुमसे’ रह जाते हैं।
– समाप्त –