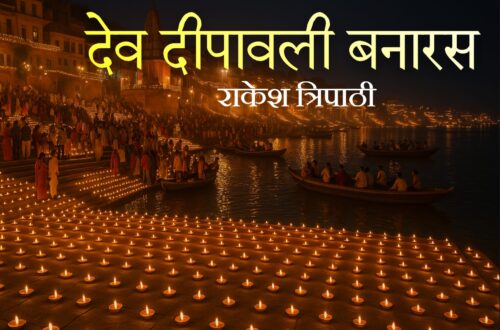नवनीत विश्वास
1
हर सुबह जैसे मुंबई जागती है – गाड़ियों की आवाज़, लोकल ट्रेनों की घरघराहट, और भीड़ के कोलाहल में – उसी के साथ एक और दुनिया भी आँखें खोलती है: डब्बावालों की दुनिया। ये वो लोग हैं जो रोज़ लाखों लोगों के घर का खाना, सैकड़ों किलोमीटर दूर, बिना एक गलती के, समय पर पहुँचा देते हैं।
नाथा पाटील, लगभग साठ साल के बुज़ुर्ग डब्बावाले, इस दुनिया के एक अनुभवी सिपाही हैं। सफेद नेहरू टोपी, हल्की झुर्रियों वाली मुस्कान, और आँखों में वर्षों का अनुभव। सुबह चार बजे उनकी नींद खुलती है, जैसे शरीर में कोई अलार्म फिट हो।
वो धीरे-धीरे हाथ-मुँह धोते हैं, चाय चढ़ाते हैं, फिर अपनी धोती कसते हैं और इस्तरी की हुई कमीज़ पहनते हैं। लकड़ी की दराज़ से वे एक छोटी सी नोटबुक निकालते हैं — जिसमें नाम, स्टेशन, गली, और डब्बों के कोड लिखे होते हैं।
उनकी साइकिल, जो अब बूढ़ी हो चली है, फिर भी उनके कदमों की सबसे पक्की साथी है।
उस सुबह, एक नया चेहरा भी साथ था — राहुल देशमुख।
नाथा का भतीजा। उम्र पच्चीस साल। स्मार्टफोन, ईयरबड्स और नए ज़माने की बातें उसके पास थीं। उसने अभी-अभी इंजीनियरिंग पूरी की थी, और अब किसी कॉर्पोरेट नौकरी की तलाश में भटक रहा था। पर आज वो नाथा के साथ था, मजबूरी में नहीं — जानने की जिज्ञासा में।
“काका, इतना सुबह कैसे उठते हो रोज़?” राहुल ने जम्हाई लेते हुए पूछा।
नाथा ने मुस्कराकर जवाब दिया, “समय पर न उठे तो डब्बा समय पर कैसे पहुँचेगा?”
राहुल को अजीब लगा — इतनी लगन, इतने पुराने काम के लिए?
चर्चगेट स्टेशन पर जैसे ही दोनों पहुँचे, वहाँ पहले से भीड़ थी। सैकड़ों डब्बावाले सफेद टोपी में, एक जैसी वर्दी में, अपने-अपने डब्बों के साथ तैयार। ट्रेनें आईं, चढ़े, उतरे, डब्बे बदले, स्टेशन बदले — पर एक बात नहीं बदली: अनुशासन।
नाथा ने एक डब्बा राहुल को पकड़ाते हुए कहा, “देख, ये डब्बा वर्ली जाना है। कोड देख — W17-PSR. W मतलब वर्ली, 17 मतलब बिल्डिंग नंबर, और PSR मतलब ग्राहक का नाम — प्रकाश संजय राणे।”
राहुल ने डब्बा उलट-पलट कर देखा, फिर पूछा, “इसमें GPS या ऐप क्यों नहीं लगाते? इतना झंझट क्यों?”
नाथा हँसे, “बेटा, ये GPS से तेज़ चलता है — भरोसे से। और ये कोडिंग, जो तू खेल समझ रहा है, हमारे लिए रोज़ की ज़िंदगी है।”
राहुल कुछ समझा, कुछ नहीं। पर डब्बे की गर्माहट, जैसे उसमें घर की खुशबू बंद हो, उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर गई।
गली-गली, बिल्डिंग-दर-बिल्डिंग, वे दोनों चलते रहे। लोग इंतज़ार करते थे — सिर्फ खाने का नहीं, अपने घर की यादों का, अपनी पत्नियों के हाथों की खुशबू का। नाथा हर बार मुस्कराते हुए डब्बा थमाते, और राहुल देखता — ये काम, महज़ काम नहीं था।
शाम को जब वे लौटे, राहुल थक चुका था।
“काका, ये काम थकाता नहीं क्या?” उसने पूछा।
नाथा मुस्कराकर बोले, “थकाता है बेटा, पर जब एक आदमी हँसकर कहे – ‘आज खाना गरम था, जैसे घर आया’ – तब सारी थकान उड़ जाती है।”
राहुल चुप हो गया।
वो नहीं जानता था कि एक डब्बा सिर्फ टिफिन नहीं होता — उसमें कोई याद, कोई रिश्ता, और कोई इंतज़ार भी बंधा होता है।
उस रात राहुल की नींद देर से आई। डब्बों के कोड, ट्रेन की आवाज़ें, नाथा की मुस्कान — सब कुछ उसके मन में घूम रहा था।
शायद कल वह फिर जाएगा।
शायद ये “अस्थायी” नहीं है।
शायद… यही कोई कहानी शुरू हो रही है।
2
राहुल अगली सुबह ठीक 4:30 बजे नाथा काका के दरवाज़े पर पहुँचा। आँखें नींद से भरी थीं, पर मन में हलचल थी। पिछली रात उसने ठीक से सोया नहीं था। नाथा के साथ बिताया पहला दिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह जो काम ‘साधारण’ समझता था, उसमें उसने एक अनुशासन देखा था, एक संवेदना, और शायद एक अदृश्य जाल जो पूरे शहर को एक-दूसरे से जोड़ता था।
“जल्दी आ गया आज?” नाथा ने चाय की प्याली बढ़ाते हुए पूछा।
“नींद ही नहीं आई,” राहुल बोला, “कल से कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ।”
नाथा मुस्कराए, “डब्बों की दुनिया में एक बार दिल लग जाए, तो फिर कुछ और अधूरा लगने लगता है।”
इस बार राहुल ने टोपी खुद पहनी। सफेद, सीधी, और गर्व के साथ।
—
चर्चगेट स्टेशन, सुबह का पहला लोकल।
आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। कुछ नए चेहरे दिख रहे थे — जिनमें से एक बुज़ुर्ग महिला थी, जो अपने बेटे के लिए रोज़ खाना भिजवाती थी।
“उसका बेटा ट्रेन ड्राइवर है,” नाथा ने बताया, “खाना उसके काम के वक्त पर जाना होता है, चाहे बारिश हो या हड़ताल।”
राहुल को हैरानी हुई, “ट्रेन ड्राइवर भी डब्बा मंगाता है?”
“बेटा, मुंबई में हर आदमी को डब्बे की ज़रूरत होती है — चाहे वो CEO हो या क्लर्क। हर डब्बा एक घर से आता है, और किसी भूखे पेट तक जाता है।”
नाथा ने उसे आज एक नया डब्बा सौंपा — D28-MSK।
“ये कहाँ जाना है?” राहुल ने पूछा।
“डोंबिवली, बिल्डिंग 28, और ग्राहक का नाम महिमा संजय कपूर,” नाथा बोले, “आज तू अकेले ले जाएगा ये।”
राहुल चौंका, “मैं? अकेले?”
“हां, सीखना है तो गलती करने से मत डर,” नाथा ने कहा, “बस एक चीज़ याद रख — डब्बा रास्ता बदल सकता है, पर समय नहीं।”
राहुल ने साइकिल ली, डब्बा हैंडल पर टांगा और चल पड़ा — अपने पहले अकेले सफ़र पर।
—
डोंबिवली की ओर
राहुल के कानों में ईयरबड नहीं थे आज। वो सुन रहा था — लोगों की बातें, गाड़ियों की आवाज़ें, ट्रैफिक की चिल्लाहट — और इन सबके बीच अपने अंदर की चुप्पी।
डब्बा बहुत हल्का था, लेकिन जैसे उसमें कोई अदृश्य भार था।
रास्ते में एक बार वह ग़लत मोड़ ले बैठा। एक अजीब-सी गली में पहुँच गया जहाँ कचरे का ढेर था, बच्चे प्लास्टिक चुन रहे थे। वहाँ खड़ा सोच ही रहा था कि एक बच्चा पास आया — “भैया, डब्बा गिरा दो क्या?”
राहुल चौंका, नीचे देखा — साइकिल का हुक ढीला हो गया था, डब्बा एक ओर झूल रहा था। उसने झट से ठीक किया, और बच्चे को एक चॉकलेट थमाई जो उसके बैग में थी।
“शुक्रिया,” उसने कहा।
बच्चा मुस्कराकर बोला, “डब्बा वाले भैया हमेशा जल्दी में रहते हैं। आप नए हो?”
राहुल मुस्कराया, “हाँ, आज पहला दिन अकेले।”
बच्चे ने उँगली से एक दिशा दिखाई, “MSK की बिल्डिंग उधर है। मेरी अम्मी वहीं झाड़ू लगाती हैं।”
—
बिल्डिंग नंबर 28
एक चार मंज़िला पुरानी बिल्डिंग, दीवारों पर सीलन, गलियों में बच्चे, और सीढ़ियों पर बैठी दो बुज़ुर्ग औरतें।
राहुल ने कोड देखा — D28-MSK — और चौथी मंज़िल पर पहुँचा।
दरवाज़ा खुला, एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। बाल गीले, आँखों में थकावट।
“महिमा संजय कपूर?” राहुल ने पूछा।
लड़की ने सिर हिलाया और डब्बा थाम लिया।
“थोड़ा लेट हो गया… पर सही सलामत है।” राहुल ने संकोच से कहा।
लड़की ने मुस्कराकर कहा, “कोई बात नहीं, डब्बा गरम है। शुक्रिया।”
राहुल जाने को मुड़ा, तो उसने पुकारा, “आप नए हैं क्या?”
“हां… आप कैसे जान गईं?”
“क्योंकि बाकी डब्बावाले मुस्कराते नहीं, बस डब्बा देकर भाग जाते हैं।”
राहुल को कुछ समझ नहीं आया। पर जैसे कुछ छू गया।
—
वापसी में…
राहुल देर से स्टेशन पहुँचा। नाथा पहले से खड़े थे, साइकिल के पास टिके हुए।
“कैसा लगा अकेले जाना?” उन्होंने पूछा।
“अलग… जैसे मैं किसी कहानी का हिस्सा बन गया हूँ,” राहुल ने कहा।
“हर डब्बा, बेटा, एक कहानी है,” नाथा बोले, “और जो उसे लेकर जाता है, वो सिर्फ संदेशवाहक नहीं — एक किरदार भी होता है।”
राहुल को याद आया लड़की की मुस्कान, बच्चा जो राह दिखा रहा था, और उस डब्बे की गरमाहट।
“आप ठीक कहते हैं, काका,” राहुल बोला, “मैं अब इसे काम नहीं, एक ज़िम्मेदारी मानता हूँ।”
नाथा की आँखों में चमक आ गई।
“शुरुआत हो गई तेरी,” उन्होंने कहा, “अब शहर तुझे अपने भीतर बुलाएगा — डब्बों के रास्ते।”
अगले दिन की सुबह फिर आने वाली थी।
लेकिन अब राहुल बदल चुका था।
3
मुंबई की सुबह फिर उसी शोरगुल से जागी। लोकल ट्रेनों की सीटी, टैक्सी की चिल्लाहटें, और सड़कों पर भागती ज़िंदगियाँ। लेकिन उस दिन राहुल कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसे इस शहर से जोड़ दिया हो।
कल का डब्बा—D28-MSK—महज एक कोड नहीं था। उस डब्बे की डोर महिमा नाम की उस लड़की से जुड़ गई थी, जिसकी आँखों में थकान थी पर लहजे में शांति।
सुबह 5:00 बजे नाथा काका के साथ राहुल चर्चगेट स्टेशन पहुँचा।
“आज फिर डोंबिवली जाएगा,” नाथा बोले, “पर आज एक और डब्बा लेना है — M28-RN।”
“RN?” राहुल ने पूछा।
“राहुल नामदेव,” नाथा ने मुस्कराकर कहा, “तेरे नाम का डब्बा।”
राहुल हँस पड़ा, “आप तो मज़ाक भी करने लगे, काका।”
“जब शागिर्द अच्छा हो, तो गुरु को भी खुशी होती है।”
डब्बे फिर से बाँटे गए। कोड जाँचे गए। ट्रेन आई। भीड़ ने धक्का दिया। और वे सब — जैसे किसी सटीक रचना का हिस्सा हों — अपनी अपनी मंज़िल की ओर रवाना हो गए।
—
राहुल फिर महिमा की बिल्डिंग पर पहुँचा।
डब्बा थामे वह सीढ़ियाँ चढ़ रहा था जब उसे दरवाज़े के पास एक लिफाफा रखा मिला — उस पर लिखा था, “डब्बावाले भैया के लिए।”
राहुल ने चौंककर इधर-उधर देखा, फिर चिट्ठी जेब में रख ली और दरवाज़ा खटखटाया।
महिमा ने आज कुछ जल्दी खोला। उसने वही हल्की मुस्कान दी।
“डब्बा वक़्त पर,” राहुल ने कहा।
“धन्यवाद,” उसने कहा, “आपका नाम?”
राहुल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, “राहुल।”
महिमा ने सिर हिलाया। चुप्पी का एक हल्का क्षण गुज़रा, फिर वह अंदर चली गई।
राहुल ने वापस साइकिल की ओर रुख किया। नीचे उतरते हुए उसने महसूस किया, किसी ने उसे सचमुच ‘चिट्ठी’ दी है — इतने डिजिटल दौर में, हाथ से लिखी चिट्ठी!
—
स्टेशन पर लौटते ही, राहुल ने चाय के ठेले के पास चिट्ठी खोली:
> “प्रिय डब्बावाले भैया,
पता नहीं ये चिट्ठी आप तक पहुँचेगी या नहीं। लेकिन आपको धन्यवाद देना था। आप जब डब्बा लाते हैं, तो मुझे लगता है जैसे घर की कोई पहचान फिर से लौट आई है।
मैं पिछले छह महीने से यहाँ अकेली हूँ। मेरे पति संजय की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। खाना बनाना तो दूर, खाने का मन भी नहीं करता था। पर मेरी सास ने ज़िद की कि मैं रोज़ घर का खाना पैक करूँ — “उसकी आदत मत तोड़,” उन्होंने कहा।
शायद इसी बहाने मैं दोबारा रसोई में लौटी। और जब आप डब्बा समय से लाकर देते हैं, तो मुझे लगता है संजय अब भी कहीं है। और मैं ज़िंदा हूँ।
आपका आभार —
महिमा”
राहुल कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी। लोकल की सीटी दूर बज रही थी। पर उसका मन उस चिट्ठी की गर्माहट में डूबा था।
उसने पहली बार समझा — डब्बा खाना नहीं, याद भी होता है।
—
अगले दिन
राहुल ने महिमा के डब्बे के साथ एक छोटा सा नोट रखा:
> “आपका पत्र पढ़ा।
मैं सिर्फ डब्बा पहुँचाता हूँ — पर अब समझा कि उसमें भावनाएँ भी होती हैं।
आप मज़बूत हैं। और आपकी रसोई संजय जी की यादों को ज़िंदा रखे हुए है।
सादर — राहुल (डब्बावाला भैया)”
नाथा ने जब देखा कि राहुल डब्बे में कुछ रख रहा है, तो मुस्कराए, “शब्दों का डब्बा है क्या?”
“कभी-कभी डब्बा सिर्फ खाना नहीं ले जाता,” राहुल बोला, “कभी-कभी संदेश भी पहुँचाता है।”
नाथा की आँखें चमक उठीं।
“अब तू सच में डब्बावाला बन गया, राहुल।”
—
महिमा को अगली सुबह चुपचाप वो चिट्ठी मिली।
उसने उसे खोला, पढ़ा, और डब्बे को थोड़ी देर तक हाथ में थामे रखा।
उस दिन उसने डब्बे में कुछ खास रखा — दो गुलाब जामुन। और एक और लिफाफा।
राहुल को जब स्टेशन लौटकर डब्बा खोलते वक्त वो मीठा मिला, तो वो मुस्कराया।
चिट्ठी खोली:
> “राहुल,
*आज मैंने पहली बार कुछ मीठा बनाया है, संजय की मृत्यु के बाद। यह बहुत साधारण है, पर शायद आप समझें कि ये मिठास सिर्फ शक्कर की नहीं है — यह जीवन की वापसी है।
धन्यवाद,
महिमा”
—
उस रात, राहुल देर तक अपनी डायरी में कुछ लिखता रहा:
> “मुंबई की रफ्तार में कुछ चिट्ठियाँ धीमी चलती हैं — पर जब पहुँचती हैं, तो जीवन को बदल देती हैं।”
उसके लिए डब्बावाला होना अब एक सेवा था, एक पुल — लोगों के बीच, दिलों के बीच, और अतीत से वर्तमान तक।
—
नाथा ने उसे देखा और सिर हिलाया।
“शहर तुझे अपना बना चुका है, राहुल।”
4
मुंबई में बारिश का मतलब होता है — देर होती ट्रेनें, जाम की कतारें, और भीगती ज़िंदगियाँ। पर डब्बावाले रुकते नहीं। बारिश, गर्मी, हड़ताल — कुछ भी हो, डब्बा समय पर पहुँचना चाहिए। यही उस व्यवस्था का धर्म है, और यही नाथा पाटील ने वर्षों से निभाया है।
उस दिन सुबह-सुबह से ही काले बादल घिरे थे। छतों पर कवेलू की छायाएँ काँप रही थीं, और लोगों की निगाहें ऊपर उठी थीं, जैसे आसमान को पढ़ना चाह रहे हों।
“आज बारिश आएगी,” नाथा ने खांसी दबाते हुए कहा।
“काका, बारिश में तो गड़बड़ होगी ना?” राहुल ने पूछा।
“गड़बड़ नहीं बेटा, तैयारी चाहिए। रेनकोट, प्लास्टिक, और मन की पकड़। आज तुझे एक नया रास्ता दिखाऊंगा — रेलवे ब्रिज के नीचे।”
राहुल चौंका, “वहाँ क्यों?”
नाथा मुस्कराए, “कुछ डब्बे सिर्फ बिल्डिंगों में नहीं पहुँचते। कुछ ज़िंदगी पटरी के किनारे भी जीती है।”
—
रेलवे ब्रिज, कुर्ला के पास
एक पुराना, जंग खाया पुल। नीचे टूटी फूटी झोपड़ियाँ, नाले के किनारे बसी ज़िंदगियाँ। वहाँ हर किसी के पास एक छाता नहीं था, पर आँखों में आशा ज़रूर थी। वहाँ भी इंसान खाना खाता था, पेट भरता था, सपने देखता था।
“यहाँ कौन सा डब्बा है?” राहुल ने पूछा।
नाथा ने एक नीली पट्टी वाला डब्बा दिखाया — KRL-RF3।
“यह डब्बा रोज़ जाता है — रामफल के लिए। वह रेलवे पुल के नीचे रहता है, पटरी के किनारे। बैंड बजाता है बारातों में, पर अब बीमार है। उसकी पत्नी घर का खाना नहीं बना सकती, तो उसका पुराना मालिक रोज़ डब्बा भिजवाता है।”
राहुल स्तब्ध रह गया।
“इतनी मेहनत सिर्फ एक बीमार आदमी के लिए?”
“नहीं बेटा, ये मेहनत भरोसे के लिए है,” नाथा बोले, “और जब इंसान की क़ीमत उसके पैसों से नहीं, उसकी याद से आंकी जाए — तब ये डब्बा और भी ज़रूरी हो जाता है।”
बारिश की पहली बूंदें गिरीं। राहुल ने जल्दी से रेनकोट पहना, डब्बा प्लास्टिक में लपेटा, और पुल के नीचे पहुँचा।
—
रामफल का चेहरा धुंधला पर ज़िंदा था।
उसकी आँखों में कमजोरी थी, पर मुस्कराहट अब भी वैसी ही थी — धीमी, मगर सच्ची।
“भैया, आज भी समय पर आ गए आप,” उसने काँपती आवाज़ में कहा।
राहुल ने डब्बा बढ़ाया, और बगल में बैठ गया।
“आपको रोज़ डब्बा कौन भेजता है?” उसने पूछा।
रामफल ने गर्दन झुकाई, “वही जिसके यहाँ मैंने बैंड बजाया था पच्चीस साल। बिन्नी साहब। जब मेरी तबियत बिगड़ी, उन्होंने मुझसे एक ही बात कही — ‘अब तू बस आराम कर, खाना मैं भेजवाऊँगा।’ और तब से ये डब्बावाले भैया रोज़ आते हैं।”
राहुल की आँखें भीग गईं — पता नहीं बारिश से या भीतर से।
“कभी मिलना हुआ उनसे?” उसने पूछा।
“नहीं,” रामफल बोले, “पर हर डब्बे में उनका आशीर्वाद लगता है।”
राहुल समझ गया — कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, आदतों से बनते हैं।
—
वापसी में
वापसी की राह बारिश से भीगी थी। ट्रेनें देरी से चल रही थीं। लोग बड़बड़ा रहे थे। मोबाइल नेटवर्क जा रहा था। सब कुछ ठहर गया था — पर डब्बे चलते रहे।
“कैसा लगा पुल के नीचे?” नाथा ने पूछा।
“जैसे ज़िंदगी की असली परीक्षा वहीं हो,” राहुल ने जवाब दिया।
“शहर का सच स्टेशन पर नहीं मिलता, बेटा,” नाथा बोले, “उसे जानना हो तो पुल के नीचे जाना पड़ता है। वहाँ इंसान छोटे दिखते हैं, पर दिल बहुत बड़े होते हैं।”
राहुल चुप रहा, जैसे वो हर शब्द को भीतर उतार रहा हो।
—
रात को राहुल ने डायरी में लिखा:
> “आज मैंने सीखा कि एक डब्बा सिर्फ खाना नहीं लाता — वह इज़्ज़त लाता है। और इज़्ज़त वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जहाँ सबसे कम बची हो।”
उसने पन्ने के किनारे लिखा: रामफल — पुल के नीचे, पर मन में ऊपर।
—
अगले दिन
राहुल फिर डब्बा लेकर रामफल के पास गया। साथ में एक छोटा सा रेडियो था, जो उसने अपने कॉलेज के दिनों से बचाकर रखा था।
“ये लीजिए,” उसने कहा, “बारिश में संगीत और भी मीठा लगता है।”
रामफल की आँखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से रेडियो को छुआ, और फिर अपने सीने से लगा लिया।
“अब खाना और अच्छा लगेगा,” उसने कहा।
—
ट्रेन की सीटी फिर बजी।
राहुल और नाथा ने फिर अपने साइकिल सम्हाली, और अगले गंतव्य की ओर बढ़ चले।
पर अब हर गंतव्य सिर्फ गली या बिल्डिंग नहीं था — अब हर जगह एक कहानी थी, एक चेहरा, एक रिश्ता।
5
हर शनिवार की शाम मुंबई के डब्बावाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। यह कोई अफसरों की बैठक नहीं होती, न ही किसी बड़ी इमारत में — बल्कि एक साधारण-सी छांव में, चर्चगेट स्टेशन के पास, जहाँ ज़मीन पथरीली है और दीवार पर वक्त की खरोंचें साफ़ दिखती हैं। इसे वे प्यार से कहते हैं — “संगठन चौकी”।
यहाँ हफ्ते भर के काम की समीक्षा होती है, नए डब्बावालों को मार्गदर्शन दिया जाता है, और सबसे ज़रूरी — साथ बैठकर चाय पी जाती है, बिना किसी दौड़ के।
राहुल के लिए यह पहली “सभा” थी। वो थोड़ा सकुचाया हुआ बैठा था, किनारे, अपने पीले झोले को गोद में रखे हुए। पास में नाथा काका खड़े थे, सिर ऊँचा, जैसे किसी पुराने योद्धा को आज अपनी सेना का नेतृत्व करना है।
“डब्बावालों की दुनिया सिर्फ गाड़ी से नहीं चलती, बेटा,” नाथा ने राहुल के कान में धीरे से कहा, “यहाँ एकता ही इंजन है।”
—
सभा शुरू हुई।
सबसे पहले आया श्रेणी सम्मान — हर उस डब्बावाले को सम्मानित किया गया जिसने पूरे हफ्ते में एक भी गलती नहीं की।
राहुल चौंका, “गलतियाँ भी गिनी जाती हैं?”
“यहाँ हर गलती एक परिवार की चिंता बन सकती है,” नाथा बोले, “अगर डब्बा गलत जगह पहुँचा, तो किसी की दवाई छूट सकती है, किसी का उपवास टूट सकता है, किसी का रिश्ता बिगड़ सकता है।”
एक वृद्ध डब्बावाला उठकर बोला, “इस बार वसई वाले शंकरभाऊ ने १०० डब्बे बिना एक भी गलती के पहुँचाए।”
सभी ने ताली बजाई। राहुल ने भी। मन में कहीं जलन नहीं, बल्कि प्रेरणा थी।
फिर आया नई पीढ़ी परिचय — जहाँ नए जुड़े डब्बावालों का स्वागत होता था।
“हमारे साथ आज पाँच नए सदस्य जुड़े हैं,” एक संयोजक ने कहा, “उनमें से एक हैं — राहुल देशमुख।”
राहुल एकदम सिहर गया। सबकी नज़र उस पर।
“आओ भैया, दो शब्द बोलो,” आवाज़ आई।
राहुल उठ खड़ा हुआ। दिल की धड़कनें तेज़।
“मैंने… मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने सोचा था ये काम छोटा है,” राहुल ने कहा, “पर यहाँ आकर समझा कि हर डब्बा एक भरोसे की चेन है। और मैं इस चेन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करता हूँ।”
तालियाँ बजीं। नाथा काका ने पीठ थपथपाई।
—
सभा के बाद चाय का दौर चला।
एक कोने में बैठा मुस्तफा चाचा, जो पिछले तीस वर्षों से डब्बा पहुँचा रहे थे, चाय की प्याली में बिस्कुट डुबोते हुए बोले, “आजकल के लड़कों में जोश तो है, बस ठहराव कम है।”
राहुल पास आ गया, “आप क्या सोचते हैं, चाचा? डब्बावाला जीवन भर किया जा सकता है?”
“क्यों नहीं,” चाचा बोले, “ये नौकरी नहीं, सेवा है। और सेवा कोई रिटायर नहीं होती।”
फिर एक बुज़ुर्ग महिला आईं, जो वहाँ चाय बनाने आती थीं। उन्होंने राहुल को देखकर कहा, “तुम वो ही हो ना जो रामफल को रेडियो दे आए?”
राहुल थोड़ा शर्माया, “जी… हाँ।”
“अच्छा किया। वो आदमी अब हर दिन रेडियो खोलकर पहले भजन सुनता है,” महिला बोलीं, “तुमने सिर्फ रेडियो नहीं दिया, उसकी सुबहें लौटा दीं।”
राहुल के गले में कुछ अटका। उसने सिर झुका लिया।
—
नाथा काका उस रात अपने घर जाते हुए बोले:
“तू अब सिर्फ मेरा भतीजा नहीं रहा, राहुल। तू इस व्यवस्था का हिस्सा बन गया है।”
“काका,” राहुल बोला, “क्या कभी आपने भी कोई गलती की है?”
नाथा रुके। लंबी साँस ली।
“एक बार… बहुत साल पहले,” वे बोले, “एक डब्बा गलत पहुँच गया। एक बुज़ुर्ग आदमी की दवा उसी डब्बे में थी। मैं देर से पहुँचा। जब पहुँचा, तब तक वो आदमी बेहोश हो चुका था। अस्पताल ले जाना पड़ा। बच गए… पर उस दिन मैंने कसम खाई कि दोबारा ऐसा नहीं होगा।”
राहुल ने देखा — नाथा की आँखों में नमी थी।
“हम इंसान हैं, गलती होती है,” नाथा बोले, “पर डब्बा जब किसी की ज़रूरत बन जाए, तब उसे समय पर पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं — कसम बन जाती है।”
—
रात को राहुल ने डायरी में लिखा:
> *“एक संगठन जो बिना मशीन, बिना ऐप्स, बिना विज्ञापन के सिर्फ विश्वास से चलता है — वह कोई साधारण चीज़ नहीं।
डब्बा जब निकलता है, तो वह सिर्फ खाना नहीं ले जाता — वह इंसानियत लेकर चलता है। और इंसानियत कभी देर से नहीं पहुँचनी चाहिए।”*
उसने नीचे लिखा:
“नाथा — सिर्फ काका नहीं, मेरी ट्रेनिंग का नक्शा।”
—
अगली सुबह रविवार था। छुट्टी का दिन।
पर राहुल देर तक सो नहीं सका।
डब्बे की दुनिया अब उसके सपनों में भी आने लगी थी — हर डब्बा एक चेहरा था, हर स्टेशन एक कहानी। और हर गलती एक भविष्य की जिम्मेदारी।
6
रविवार की सुबह मुंबई कुछ देर से उठती है। लोकल ट्रेनों की रफ्तार सुस्त होती है, स्टेशन खाली-से लगते हैं, और चाय के ठेलों पर अख़बारों की गड्डियाँ बिना जल्दी के खुलती हैं। पर डब्बावालों के लिए रविवार एक खास दिन होता है — जब डब्बा नहीं पहुँचाया जाता, पर कहानियाँ पहुँचती हैं।
उस दिन राहुल की नींद जल्दी खुल गई। खिड़की के बाहर से आती हल्की धूप, और दूर से आती समंदर की आवाज़ — जैसे कोई पुरानी कविता की पंक्तियाँ हों। लेकिन उसका मन एक ही नाम में अटका था — महिमा।
पिछले हफ्तों में महिमा से जितनी चिट्ठियाँ आई थीं, उतनी ही चुप्पियाँ भी थीं। उनका रिश्ता संवादों से नहीं, संकेतों से बन रहा था — हर डब्बे के साथ एक मिठाई, हर लिफाफे में एक शब्द, और हर मौन में एक पुकार।
रविवार को राहुल ने तय किया कि वह महिमा से मिलने जाएगा — बिना डब्बा, बिना टोपी, सिर्फ अपने आप को लेकर।
—
डोंबिवली — दोपहर 12 बजे
राहुल जब महिमा की बिल्डिंग पर पहुँचा, तो पहली बार उसने खुद को डब्बावाला नहीं, एक आगंतुक की तरह महसूस किया। हाथ में कोई झोला नहीं था, पर दिल में थोड़ी घबराहट ज़रूर थी।
उसने दरवाज़ा खटखटाया।
महिमा ने दरवाज़ा खोला तो थोड़ी चौंकी। वह आज सलवार-सूट में थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर बिना थकान के ताजगी।
“आप?” उसने पूछा।
“मैं… आज डब्बा नहीं लाया,” राहुल ने हँसने की कोशिश की, “बस मिलने आया था।”
महिमा थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर बोली, “अंदर आइए।”
—
घर के भीतर एक सादगी थी।
दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ एक छोटी अलमारी, एक जलता दिया, और पास रखी संजय की पुरानी फोटो — एक फ्रेम में, थोड़ा धुंधला।
“चाय पीएंगे?” महिमा ने पूछा।
“ज़रूर।”
जब वह रसोई में गई, राहुल की नज़र पास रखे एक डायरी पर पड़ी। खोलना नहीं चाहता था, पर नाम लिखा था — “संजय की आवाज़ें”।
महिमा लौटी और डायरी की ओर देखकर बोली, “वो संजय की कविताएँ हैं। जब वे जिंदा थे, तो हर रविवार कुछ लिखते थे — खुद के लिए, मेरे लिए।”
“आपने उन्हें सहेज कर रखा,” राहुल बोला।
“हाँ,” उसने कहा, “जैसे डब्बे में खाना रखते हैं — ध्यान से, धीरे से।”
—
चाय की प्याली के साथ एक बातचीत शुरू हुई।
“आपने कभी सोचा था कि किसी डब्बावाले से चिट्ठियाँ लिखेंगी?” राहुल ने मुस्कराकर पूछा।
महिमा ने सिर झुकाया, “नहीं। पर कभी-कभी सबसे गहरी बातें उन्हीं से होती हैं, जो हमारे सबसे करीब न हों — बस सबसे सच्चे हों।”
“और आप?” उसने अचानक पूछा, “आपने कभी किसी को इस तरह जवाब दिया था?”
“पहली बार,” राहुल बोला, “पहली बार लगा कि मेरी साइकिल की घंटी से किसी का मन भी जाग सकता है।”
दोनों चुप हो गए। बारिश की फुहारें खिड़की से दिखने लगी थीं।
—
फिर महिमा ने कहा:
“क्या आप संजय की एक कविता सुनना चाहेंगे?”
राहुल ने सिर हिलाया। वह कुछ नहीं कह सका।
महिमा ने डायरी से एक पन्ना खोला। उसका स्वर धीमा था, पर साफ़:
> *“मैं डब्बे में बाँधता हूँ घर की बास,
दाल में छुपा रखता हूँ अपनी सांस।
जब तुम खाओ, समझो —
मैं हर निवाले में साथ हूँ,
भले ही शाम को लौट न सकूँ।”*
राहुल की आँखें नम हो गईं। उसने अपनी नज़रों को चाय की प्याली में छुपा लिया।
“उन्होंने ये उस महीने लिखी थी,” महिमा बोली, “जब पता चला उन्हें लीवर की बीमारी है।”
“आपने कभी नया जीवन शुरू करने का सोचा?” राहुल ने संकोच से पूछा।
महिमा थोड़ी देर चुप रही। फिर बोली, “मैं हर दिन कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते — वो बस एक शक्ल बदलते हैं।”
“और मैं?” राहुल ने धीमे से पूछा।
महिमा की आँखें उससे मिलीं, फिर फिसल गईं खिड़की की ओर। बाहर बारिश तेज़ हो गई थी।
“आप अभी जीवन के उस मोड़ पर हैं, जहाँ सवाल ज़्यादा हैं। जवाबों के लिए वक़्त लगेगा,” उसने कहा।
राहुल मुस्कराया, “पर कुछ सवाल पूछना ज़रूरी होता है, नहीं?”
“हाँ,” महिमा बोली, “पर हर उत्तर पाने की ज़िद भी नहीं करनी चाहिए।”
—
शाम को जब राहुल लौट रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि आज उसने डब्बा नहीं पहुँचाया, लेकिन एक रिश्ता ज़रूर छुआ था — नज़दीक नहीं, लेकिन सम्मानपूर्वक।
रास्ते में एक फूलवाले की दुकान से उसने गुलाबी गुलाब खरीदा — छोटा, सादा, बिना रिबन के।
—
अगली सुबह
राहुल ने महिमा के डब्बे में एक छोटा लिफाफा रखा। उसमें लिखा था:
> *“कुछ रिश्ते सिर्फ संवादों से नहीं, मौन से भी बनते हैं।
उस कविता के लिए धन्यवाद —
आपने सिर्फ शब्द नहीं सुनाए, एक आत्मा से मिलाया।”*
साथ में वही गुलाबी गुलाब रखा था।
—
महिमा ने जब डब्बा खोला, तो चौंकी नहीं।
उसने बस गुलाब को पास रखे संजय की तस्वीर के नीचे रखा, और मुस्कराई — बहुत धीमे, बहुत भीतर से।
7
मुंबई की लोकल ट्रेनें जैसे हर चेहरे को अपने भीतर समेट लेती हैं। कोई किनारे बैठा है खिड़की से बाहर देखते हुए, कोई खड़ा है मोबाइल में गुम, और कोई खड़ा-खड़ा ही नींद ले रहा है। पर कभी-कभी, इन ट्रेनों में ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मिलने की कोई योजना नहीं होती — बस नियति तय करती है।
उस दिन राहुल चर्चगेट से कुर्ला के लिए निकला था। समय था दोपहर 12:10 की ट्रेन। डब्बा हाथ में था — KRL-VP12 — यानी वसंत पाटिल के लिए।
नाथा काका ने आज छुट्टी ली थी — पुरानी कमर में अकड़न थी। राहुल अकेला ही निकला था।
—
ट्रेन भीड़ से भरी नहीं थी, पर खाली भी नहीं। राहुल खिड़की के पास बैठा था, डब्बे को अपनी गोद में टिकाए। तेज़ हवा बाहर के मौसम को भीतर ला रही थी। स्टेशन दर स्टेशन लोग चढ़ते-उतरते गए।
कुर्ला से पहले, ट्रेन थोड़ी देर के लिए एक जगह अटक गई — रेलवे सिग्नल के कारण। यह आम बात थी। लेकिन तभी राहुल के सामने वाली सीट पर एक बुज़ुर्ग आदमी आकर बैठे। सफेद कुरता, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, और आँखों में कोई ऐसा सन्नाटा जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते।
वे चुपचाप राहुल को देखते रहे। राहुल ने आदतन मुस्कुराकर सिर झुकाया।
“डब्बा पहुँचा रहे हो?” उन्होंने पूछा।
“जी हाँ,” राहुल बोला, “डब्बावाला हूँ।”
“मैं भी था,” बुज़ुर्ग ने कहा, “आज से चालीस साल पहले।”
राहुल का ध्यान एकदम खिंच गया।
“सच में?” उसने पूछा, “कहाँ काम किया आपने?”
“मलाड से बांद्रा लाइन पर,” उन्होंने उत्तर दिया, “जब मैं जवान था, तो रोज़ 60 डब्बे पहुँचाता था — साइकिल पर, बारिश में, बिना मोबाइल के।”
राहुल ने पूछा, “फिर छोड़ क्यों दिया?”
वे कुछ देर खामोश रहे। ट्रेन धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी।
“एक दिन डब्बा गुम हो गया,” वे बोले, “वो एक बच्ची का था — स्कूल में लंच के समय जब वह डब्बा नहीं पहुँचा, तो बच्ची रोती रही। बाद में पता चला, वह डब्बा गलत स्टेशन पर चला गया था। कोई बड़ी बात नहीं थी शायद — पर मुझे लगा कि मैंने किसी मासूम का भरोसा तोड़ दिया।”
“फिर?” राहुल ने पूछा।
“मैं टूट गया,” बुज़ुर्ग बोले, “संगठन ने कहा, ‘गलती हो जाती है।’ पर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया। और नौकरी छोड़ दी।”
राहुल चुप हो गया।
“अब क्या करते हैं आप?” राहुल ने धीरे से पूछा।
“कुछ नहीं,” बुज़ुर्ग हँसे, “ज़िंदगी अब सिर्फ देखती है, दौड़ती नहीं। पर जब तुम्हें देखा डब्बा लेकर, तो पुरानी यादें लौट आईं।”
राहुल ने डब्बा दिखाया, “यह वसंत पाटिल के लिए है। कुर्ला ब्रिज के पास।”
बुज़ुर्ग की आँखें थोड़ी चमक उठीं, “वसंत? अगर वही है जिसे मैं जानता हूँ, तो वो कभी मेरे साथ काम करता था। उसके घर के पास एक नीम का पेड़ है, और खिड़की से हर सुबह उसकी पत्नी तुलसी में पानी डालती है।”
राहुल को आश्चर्य हुआ, “आपको सब याद है?”
“जो बातें दिल को छू जाती हैं, वो भूलती नहीं,” उन्होंने कहा।
—
ट्रेन कुर्ला पहुँची।
राहुल उतरने लगा, तो बुज़ुर्ग बोले, “मैं भी उतरूँगा, चलो साथ।”
राहुल और वे दोनों स्टेशन की सीढ़ियाँ पार करते हुए पुल के नीचे पहुँचे — वही वसंत पाटिल का इलाका।
जैसे ही राहुल ने दरवाज़ा खटखटाया, एक अधेड़ महिला ने दरवाज़ा खोला।
“डब्बा…” राहुल ने कहा, पर उससे पहले ही बुज़ुर्ग पीछे से बोले, “शांता… पहचानती है मुझे?”
महिला ने जैसे भूत को देखा हो।
“विलास?” वह काँपते स्वर में बोली।
“हां, मैं… लौट आया,” उन्होंने धीरे से कहा।
राहुल हैरान खड़ा रहा। यह तो कहानी से बढ़कर कुछ था।
शांता की आँखें नम हो गईं, “तुमने इतने सालों में कोई खबर क्यों नहीं दी?”
“खुद से नज़रें नहीं मिला पाया,” विलास बोले।
उसने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया।
—
राहुल चुपचाप वह डब्बा नीचे रखकर वापस मुड़ा।
पीछे कोई आवाज़ नहीं दी। कुछ मिलन शब्दों के बिना ही पूरे हो जाते हैं।
जब वह वापस स्टेशन की ओर लौट रहा था, उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे — क्या एक गलती इंसान की पूरी पहचान तय कर सकती है? क्या आत्मग्लानि सबसे बड़ा अकेलापन है?
—
वह उसी ट्रेन से लौट रहा था, अकेले। लेकिन आज उसकी गोद में डब्बा नहीं था — बल्कि कुछ और भारी था। शायद एक अधूरी कहानी का अंत… या एक नई शुरुआत।
उसने जेब से अपनी डायरी निकाली, और लिखा:
> *“हम डब्बे पहुँचाते हैं, पर कभी-कभी डब्बा हमें भी पहुँचाता है — किसी अजनबी की स्मृति तक, किसी भूले रिश्ते के मोड़ तक।
आज ट्रेन में बैठा एक अजनबी मेरे भीतर उतर गया — अपने बोझ के साथ, और माफी के बिना भी स्वीकार किए गए प्यार के साथ।”*
—
रात को, जब राहुल घर पहुँचा, तो उसने नाथा काका को फोन लगाया।
“काका,” वह बोला, “आज एक पुराने डब्बावाले से मिला — जिसने गलती के डर से सब छोड़ दिया।”
“नाम क्या था?” नाथा ने पूछा।
“विलास…”
फोन के उस पार चुप्पी छा गई।
“विलास कदम?” नाथा की आवाज़ काँपी।
“हां… आप जानते हैं?”
“बहुत अच्छे से,” नाथा बोले, “हम साथ काम करते थे। उसके जाने के बाद संगठन में जैसे एक छेद रह गया था। वह गलतियाँ नहीं करता था — सिर्फ बहुत ज्यादा सोचता था।”
“आज वह वापस वसंत पाटिल के घर गया,” राहुल बोला, “और शांता नाम की महिला ने उसे पहचान लिया।”
“फिर से एक डब्बा जुड़ गया,” नाथा ने कहा।
“हां, काका,” राहुल ने धीरे से कहा, “कभी-कभी डब्बा रास्ता बदल देता है — लेकिन मंज़िल फिर भी मिलती है।”
8
मुंबई की हवा में अक्टूबर का स्पर्श था — न ज़्यादा गर्म, न ठंडी, बस एक थकान के बाद की साँस जैसी। स्टेशन पर लोगों की रफ्तार अब भी वैसी ही थी, पर राहुल के लिए हर स्टेशन अब पहचान भरा था।
वह अब सिर्फ एक डब्बावाला नहीं था, वह इन गलियों और ट्रेनों का साक्षी बन चुका था — महिमा की चिट्ठियाँ, रामफल की रेडियो पर गूंजती धुनें, विलास की वापसी, और अब… उसका अपना रास्ता।
—
रविवार की एक खास सुबह, राहुल को नाथा काका का फोन आया।
“आज संगठन की वार्षिक बैठक है,” नाथा ने कहा, “हर डब्बावाले की मौजूदगी ज़रूरी है — और तेरी सबसे ज़्यादा।”
“मैं वहाँ रहूंगा,” राहुल ने कहा, “पर क्या कुछ अलग होने वाला है?”
नाथा ने हँसकर कहा, “बहुत कुछ।”
—
वह ‘संगठन चौकी’ की जगह आज बदल गई थी।
बैठक इस बार दादर के एक पुराने हॉल में थी — जहाँ कभी ब्रिटिश काल में रेलवे अधिकारी बैठते थे, वहीं अब सैकड़ों डब्बावाले अपनी टोपी में गर्व लेकर बैठे थे। मंच पर एक बड़ी टेबल थी, और उसके पीछे कई वरिष्ठ सदस्य।
राहुल को पहली बार मंच के पास बैठाया गया।
“मुझे क्यों बुलाया गया आगे?” राहुल ने पूछा।
“तू समझेगा,” नाथा ने मुस्करा कर कहा।
—
बैठक शुरू हुई।
सबसे पहले पुराने सदस्यों को सम्मानित किया गया — पचास साल सेवा में रहे वसई के दादा, फिर पुणे से आए एक बुज़ुर्ग जो अब रिटायर हो चुके थे। हर नाम के साथ तालियाँ गूंजीं।
फिर मुख्य संयोजक उठे — एक शांत-स्वर में बात करने वाले व्यक्ति, जिनके चेहरे पर अनुभव की गहराई थी।
“इस साल हमने सिर्फ डब्बे नहीं पहुँचाए,” उन्होंने कहा, “हमने कहानियाँ भी उठाईं — और उन्हें समय से पहुँचाया।”
फिर उनकी आँखें राहुल पर पड़ीं।
“और इस साल हम एक नए सदस्य को विशेष सम्मान देना चाहते हैं,” उन्होंने कहा, “एक ऐसा युवा जिसने डब्बे की गरिमा को सिर्फ अपने कर्म से नहीं, अपने दृष्टिकोण से भी जिया है। जिसने हमें यह याद दिलाया कि हर डब्बा सिर्फ खाना नहीं — विश्वास, यादें, और जीवन की एक रेखा होता है।”
राहुल स्तब्ध था।
“हम राहुल देशमुख को संगठन की ‘युवा विरासत प्रतिनिधि’ के रूप में मनोनीत करते हैं — जो आने वाली पीढ़ी को यह बताएगा कि डब्बावाला होना सिर्फ एक काम नहीं, एक दर्शन है।”
तालियाँ बजीं। राहुल मंच पर बुलाया गया। एक टोपी उसके सिर पर रखी गई — पारंपरिक गांधी टोपी, जिसके कोने पर संगठन का प्रतीक चिह्न कढ़ा हुआ था।
—
राहुल की आँखें नम थीं।
उसने माइक थामा।
“मैंने जब यह काम शुरू किया, तब सोचा था कि बस डब्बे उठाने हैं, जगह पर पहुँचाने हैं,” राहुल बोला, “पर फिर मैंने महसूस किया — मैं किसी की माँ की रसोई की खुशबू लेकर जाता हूँ, किसी बीमार के लिए दवा का डिब्बा बन जाता हूँ, और कभी किसी विधवा की यादों का संदूक भी हूँ।”
“महिमा की चिट्ठियों ने मुझे सिखाया कि खाना सिर्फ भूख के लिए नहीं, स्मृति के लिए भी होता है। रामफल ने दिखाया कि सेवा वहाँ सबसे ज़रूरी होती है जहाँ नाम नहीं पहुँचता। विलास जैसे लोगों ने बताया कि कभी-कभी एक गलती पूरी ज़िंदगी रोक देती है — पर लौटना हमेशा संभव है।”
उसके शब्दों में कंपन था।
“और आज अगर मैं कुछ हूँ, तो नाथा काका की वजह से। उन्होंने मुझे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया — उन्होंने मुझे ‘मानवता’ में विश्वास दिलाया।”
पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियाँ गूंजने लगीं।
—
बैठक के बाद
नाथा ने राहुल को गले से लगाया।
“अब तू आगे बढ़ेगा,” काका बोले, “मैंने अपना समय जी लिया। अब तू डब्बे से किताब लिखेगा।”
“क्या मतलब?” राहुल चौंका।
नाथा ने मुस्कराकर एक पुरानी डायरी निकाली — डब्बों की कहानियाँ — जो उन्होंने तीस सालों तक चुपचाप लिखी थी।
“यह मेरी विरासत है, बेटा,” उन्होंने कहा, “अब तू इसे आगे बढ़ा।”
राहुल ने वह डायरी हाथ में ली — उसमें पहले ही पन्ने पर लिखा था:
> *“हर डब्बा एक कहानी है।
और हर कहानी एक दिन अपने लेखक को ढूंढ़ ही लेती है।”*
—
एक साल बाद —
राहुल ने वह किताब “डब्बे के रास्ते” के नाम से प्रकाशित की। उसमें हर अध्याय एक व्यक्ति की कहानी थी — महिमा, रामफल, विलास, शांता, और उस पुल के नीचे बजता रेडियो।
किताब खूब पढ़ी गई। न केवल डब्बावालों ने, बल्कि आम लोगों ने भी।
मुंबई की लाइब्रेरी में एक लड़की ने वह किताब पढ़ते हुए अपने दोस्त से कहा, “ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये शहर की धड़कन है।”
—
महिमा ने भी वह किताब पढ़ी।
उसने राहुल को एक चिट्ठी भेजी:
> *“राहुल, अब जब तुम्हारी कहानियाँ सब तक पहुँच गई हैं,
क्या अब तुम मेरे लिए एक और डब्बा लाओगे —
जिसमें हो सिर्फ ‘समय’ — बैठने, साथ चाय पीने, और कुछ न कहने का?”*
राहुल ने जवाब में सिर्फ एक पंक्ति लिखी:
“अब हर रविवार सिर्फ मेरे लिए नहीं — हमारे लिए होगा।”
अंतिम दृश्य
राहुल एक ट्रेन में बैठा है, खिड़की के पास। साइकिल स्टेशन पर टिकी है। गोद में डब्बा नहीं है — हाथ में किताब है। सामने बैठी महिमा, मुस्कराती है। ट्रेन चलने लगती है।
खिड़की से हवा आती है।
और शहर… वही है। मगर अब, हर डब्बा किसी न किसी को जोड़ रहा है।
विरासत जारी है।
(समाप्त)