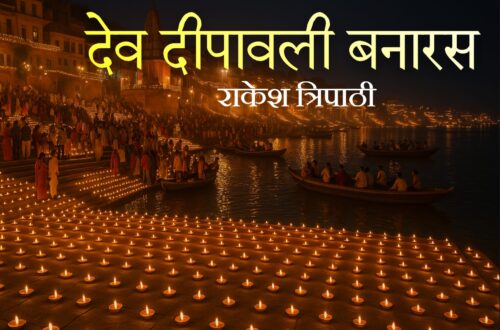विराज देशमुख
अध्याय १
दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस की सड़कें अगस्त की हल्की बारिश से चमक रही थीं। पेड़ों की पत्तियाँ भीग चुकी थीं, और हॉस्टल के गलियारों में एक नई उमंग घुली हुई थी—नए सेमेस्टर की, नई क्लासेस की, और हाँ, नए चेहरों की भी। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एक छोटा-सा जमावड़ा था, हाथों में पोस्टर, गले में स्लोगन, और आँखों में जुनून। काव्या, अपने कुर्ते के नीचे एक पुराने से झोले में नोटबुक और पेन लिए, उस भीड़ के बीच खड़ी थी—ना पीछे, ना आगे—बस ठीक वहीं जहाँ सबसे ज्यादा आवाज़ गूंजती थी। “आज की नारी सब पर भारी!” उसका गला फटने को था, लेकिन आवाज़ काँपी नहीं। वह सामाजिक न्याय, शिक्षा में समानता और जातीय भेदभाव के खिलाफ़ आवाज़ उठा रही थी। और यहीं, ठीक सामने, भीड़ से थोड़ी दूर, खड़ा था अमन—एक अलग तरह की नज़रों से उसे देखता हुआ। कोई विशेष आकर्षण नहीं, ना ही फिल्मी किस्म की पहली नजर वाला असर। बल्कि उसे हैरत हो रही थी—कोई इतनी उग्रता से, इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकता है और फिर भी भीतर से इतना शांत दिख सकता है? अमन को लगा जैसे ये लड़की सिर्फ़ बहस नहीं कर रही, किसी पुराने घाव को कुरेद रही है।
अमन, जो हिस्ट्री का छात्र था और अक्सर कैंपस की राजनीति से दूरी बनाए रखता था, उस दिन काव्या के शब्दों में कुछ ऐसा महसूस कर बैठा जो किताबों की स्याही से परे था। उसने देखा कि कैसे लोग उसकी बातों पर तालियाँ बजा रहे थे, लेकिन वह खुद किसी तालियों की मोहताज नहीं थी। उसकी आँखें वहाँ कहीं नहीं थीं—वो तो जैसे खुद से ही लड़ रही थी। अमन को ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हों—उसे लगता था ये सब ‘हाइपर रिएक्टिव’ लोग होते हैं। पर काव्या में कुछ था—शायद उसकी बेबाकी, या शायद वो टूटन जो उसके आत्मविश्वास में कहीं छिपी थी। अगले दिन दोनों की क्लास पॉलिटिकल थ्योरी में साथ पड़ गई। प्रोफेसर ने जब सवाल पूछा कि “क्या असहमति देशविरोधी हो सकती है?” तो काव्या ने तुरंत हाथ उठाया और तीखे शब्दों में जवाब दिया। अमन को लगा कि अब तो बात छेड़नी ही पड़ेगी। उसने क्लास के बाहर उसे टोका—“इतनी नफरत भरकर बोलती हो, क्या कभी किसी और नजरिये से देखना सीखा है?” काव्या ने बिना पलटे जवाब दिया—“नफरत से नहीं, अनुभव से बोलती हूँ। और हाँ, तुम्हारी तरह चुप रहना नहीं सीखा।” बस वहीं से एक बहस की शुरुआत हुई, जो अगले कई हफ्तों तक लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और कैंपस के कोनों में चलती रही। दोनों की दुनिया अलग थी—एक तर्क के सहारे लड़ती, दूसरी तर्क को तोलती थी।
उनकी मुलाकातें योजनाबद्ध नहीं थीं, लेकिन टकराव जैसे नियति बन चुका था। किसी दिन डिबेट हॉल में, किसी दिन एंट्री गेट के पास पोस्टर के बगल में खड़े—दोनों के बीच बातें कम और बहसें ज्यादा होती थीं। लेकिन उन बहसों में कुछ अजीब-सा अपनापन था, जैसे दोनों को भरोसा हो कि दूसरा जवाब देगा, और फिर भी वही बात फिर से शुरू की जाएगी। काव्या को अमन की गहराई पसंद आने लगी थी, भले ही वह उससे असहमत रहती। अमन को काव्या की आग में छिपी संवेदनशीलता नजर आने लगी थी, भले ही वह उस आग में जलने से डरता था। प्रोफेसर सुरभी सेन को भी यह अजीब-सी केमिस्ट्री दिखने लगी थी—वह अक्सर मजाक में कहतीं, “अगर ये दोनों एक ही दिशा में सोचना शुरू कर दें, तो क्रांति हो जाए।” मगर दोनों को समझ में नहीं आता था कि ये बहसें कब धीरे-धीरे समझदारी में बदलने लगीं, और समझदारी कब भावनाओं के दरवाज़े तक पहुँच गई। उस समय वे नहीं जानते थे कि एक दिन जंतर मंतर की एक लंबी रात, उनकी सोच, उनका विरोध और शायद उनका दिल भी बदल देगी। उस रात से पहले, वे सिर्फ एक-दूसरे के शब्दों को सुनते थे—उसके बाद, शायद पहली बार, उन्होंने एक-दूसरे की ख़ामोशी सुनी।
अध्याय २
सितंबर की शुरुआत थी। विश्वविद्यालय में चुनाव की हलचलें हवा में गूंजने लगी थीं। हर गली, हर खंभा, हर दीवार किसी संगठन का झंडा या पोस्टर उठाए खड़ी थी। कैंपस का डिबेट हॉल भी उसी जोश में रंगा हुआ था। आज का मुद्दा था: “राष्ट्र और असहमति—क्या दोनों साथ चल सकते हैं?”। काव्या, प्रतिनिधित्व कर रही थी एक वामपंथी छात्र संगठन की ओर से, और अमन, राष्ट्रवादी विचारधारा के छात्र मंच से। हॉल खचाखच भरा था। फरहा कैमरे के पीछे थी, हर बयान, हर चेहरा कैद कर रही थी। अनिरुद्ध, पहली पंक्ति में बैठा, अमन को आँखों से ताकीद दे रहा था—”संयम मत खोना, ये लोग भड़काते हैं।”
डिबेट शुरू हुई और काव्या ने माइक थामते ही सीधे बात रख दी—”अगर देश एक माँ है, तो क्या माँ अपने बच्चों की बात सुनना बंद कर देती है? असहमति देश के खिलाफ नहीं, उसके लिए होती है!” उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, और शब्दों में आग। दर्शकों की एक लहर उसके समर्थन में उठी। फिर आया अमन का नंबर। वह धीमे, गूढ़ स्वर में बोला—”राष्ट्र कोई मैदान नहीं, जहाँ हर कोई अपनी मर्जी से चीख-चिल्ला सके। राष्ट्र जिम्मेदारी है, अनुशासन है। देश को गाली देकर कोई क्रांति नहीं आती, वह सिर्फ़ दूरी लाती है—दिलों में और ज़मीन पर भी।” उसकी बात खत्म हुई तो सन्नाटा था—फिर तालियाँ बजीं, अलग पंक्तियों से।
डिबेट खत्म होते-होते बात बहस से तंज में और तंज से आरोप में बदल गई। काव्या ने एक पल के लिए अमन को चुनौती भरे स्वर में कहा—”तुम इतिहास पढ़ते हो न, तो पढ़ना—क्रांतियाँ तालियों से नहीं, सवालों से होती हैं। और जिनके पास सवाल नहीं, वो अक्सर व्यवस्था के पालतू बन जाते हैं।” अमन ने गहरी सांस ली, आँखें नीची कीं, फिर कहा—”कभी-कभी ज़्यादा सवाल करने वाले खुद सवाल बन जाते हैं। और जब जवाब देना पड़ता है, तब सब कुछ ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी’ बन जाता है।” यह सुनते ही हॉल में फिर से खलबली मच गई। लेकिन उस पल, दोनों की आँखों में तकरार से ज़्यादा कुछ और था—एक जिद, एक अदृश्य खिंचाव। डिबेट खत्म हुआ, पर दिलों की बहस अब शुरू हुई थी, और उसके अंत का कोई तय मंच नहीं था।
अध्याय ३
दिल्ली विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी अपने विशाल गलियारों, पुरानी लकड़ी की मेज़ों और ऊँची छतों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने सन्नाटे के लिए। वहाँ हर कदम की आवाज़ गूँजती थी, हर पन्ना पलटने की सरसराहट एक संवाद लगती थी। काव्या अक्सर दोपहर के समय लाइब्रेरी के उस कोने में बैठती थी जहाँ की खिड़की से गुरुद्वारे का झंडा दिखता था। उसकी डायरी हमेशा खुली रहती, जैसे किसी न दिखने वाली ताक़त से बातें कर रही हो। वह आंदोलनों पर रिसर्च कर रही थी—नक्सलबाड़ी से लेकर शाहीन बाग़ तक की आवाज़ों की पड़ताल कर रही थी। उसी कोने में, लेकिन कुछ दूर, अमन भी बैठा करता था—इतिहास की किताबों में गुम, तथ्यों और घटनाओं की तह में उतरता हुआ। वे एक-दूसरे को जानबूझकर नजरअंदाज़ करते, मगर उनकी मौजूदगी हर वाक्य में शामिल होती।
एक दिन अमन ने देखा कि काव्या की नोटबुक खुली है और उसमें लिखा है—”इंकलाब सिर्फ़ नारों से नहीं, रिश्तों की गहराई से भी आता है।” वह चौंका, क्योंकि यह एकदम वैसी ही बात थी जैसी वह सोचता था लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसने मन ही मन तय किया कि आज बात करेगा। वह धीरे-धीरे उसके पास गया, और धीरे से बोला—”तुम जो लिखती हो, उससे ज़्यादा सुना जाता है, जितना तुम बोलती हो।” काव्या ने सिर उठाया, पहले थोड़ी हिचकी, फिर कहा—”तुम जो चुप रहते हो, वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें इरादा छिपा होता है।” फिर भी, उनकी आँखों में पहली बार कुछ नर्म सा उतर आया था। बहस की तल्ख़ी अब बातचीत की शक्ल लेने लगी थी। अगले कुछ दिनों में किताबों की अदला-बदली शुरू हुई—कभी फैज़ की शायरी की किताब, कभी दिनकर की कविताओं का संकलन।
विचारों की खींचतान बनी रही, लेकिन अब उनके बीच एक नज़र थी जो कभी-कभी किताब से ज़्यादा बोल जाती। एक बार अमन ने काव्या से पूछा—”तुम इतनी आवाज़ उठाती हो, कभी थकती नहीं?” काव्या ने बिना सोचे जवाब दिया—”थकती हूँ, लेकिन रुकना डराता है।” वह जवाब अमन के भीतर कहीं गहराई तक बैठ गया। लाइब्रेरी की दीवारों ने देखा कि दो विरोधी विचारों वाले लोग एक-दूसरे को पढ़ने लगे हैं, किताबों से हटकर, साँसों और चुप्पियों के बीच। उन्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि वे एक नई भाषा गढ़ रहे हैं—जिसमें बहसें थीं, लेकिन कटुता नहीं; असहमति थी, लेकिन दूरी नहीं। यही लाइब्रेरी, जो कभी तटस्थ थी, अब उनकी अनकही कहानी की मूक गवाह बन चुकी थी।
अध्याय ४
अक्टूबर की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। दिल्ली की हवा में अब हलकी सी नमी और मोहब्बत का एक अनकहा सा इत्र घुलने लगा था। यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग ने एक एक्सकर्शन ट्रिप का आयोजन किया—दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत पर। जगहें थीं—हुमायूं का मकबरा, चांदनी चौक की हवेलियाँ और पुरानी दिल्ली की गलियाँ। अमन और काव्या दोनों इस ट्रिप में शामिल थे, शायद एक-दूसरे को बिना बताए, सिर्फ़ उम्मीद में कि शायद वो भी आएगा। सफर की शुरुआत बस में चुपचाप हुई। अमन खिड़की के पास बैठा था, हाथ में नोटबुक, और काव्या पीछे की सीट पर फरहा के साथ। दोनों की नजरें बार-बार एक-दूसरे को ढूंढ़तीं, टकरातीं, फिर हट जातीं। चांदनी चौक पहुँचे तो एक पुरानी मिठाई की दुकान पर सब रुके। काव्या ने इमरती का ऑर्डर दिया, और जैसे ही उसने सामने देखा, अमन वही खड़ा था, अपने हाथ में जलजीरा लिए। दोनों मुस्कराए—पहली बार बिना किसी बहस के, बिना शब्दों के।
हुमायूं के मकबरे में, लाल पत्थरों की छाया और मीनारों के बीच, काव्या अकेली टहल रही थी। अमन ने देखा और पास आकर बोला—“इतिहास की इमारतें भी तुम्हें उतनी ही गहराई से खींचती हैं जितना तुम्हारी बातें।” काव्या चौंकी, लेकिन फिर धीरे से बोली—“क्योंकि ये भी गवाही देती हैं, चुप रहकर।” दोनों साथ-साथ चलने लगे, पुराने फव्वारों और झरोखों के बीच, बिना ज्यादा बोले। उन्हें लगा जैसे शहर की ये पुरानी दीवारें उनका अतीत नहीं, बल्कि उनके भीतर की बेचैनियों को सहेज रही हैं। बाद में, लौटते समय, बस में जगह कम थी, और अमन ने काव्या के पास बैठने की हिम्मत की। बातचीत में कविता आ गई, और दोनों ने महसूस किया कि शब्दों के बाहर भी कुछ जुड़ने लगा है—जैसे कोई लंबी बहस अब एक नर्म संवाद में ढलने लगी हो।
लेकिन शाम को जब सब इंडिया गेट के पास ठहरे, कुछ छात्र राजनीतिक नारे लगाने लगे। उनमें से कुछ ने काव्या पर कटाक्ष किए—“वामपंथी मोहब्बत अब राष्ट्रवाद से समझौता कर रही है?” और अमन से—“तू अब क्या ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के साथ घूमेगा?” हवा में तनाव घुल गया। काव्या का चेहरा उतर गया, और अमन की मुट्ठियाँ भींच गईं। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर काव्या ने सख्त लहजे में कहा—“तुम्हें जो सही लगे, वो चुन सकते हो, पर मेरे साथ खड़े होने के लिए तुम्हें खुद को खोना नहीं पड़ेगा।” अमन ने जवाब नहीं दिया, बस दूर देखता रहा। पहली बार, दोनों ने नज़दीकी के साथ दूरी भी महसूस की—दिल तो जुड़ने लगे थे, पर विचारों की दीवार अब भी अडिग थी। उस दिन दिल्ली की गलियाँ उनके दिलों के रास्तों का आईना बन गईं—जो कभी पास लाती थीं, तो कभी सवालों से उलझा देती थीं।
अध्याय ५
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी थी, और इसके कारण शहर का माहौल गहमागहमी में डूबा हुआ था। सरकार की नई नीतियों के खिलाफ़ एक विशाल आंदोलन की योजना बनाई गई थी, और जंतर मंतर पर लाखों छात्रों और युवाओं का जमावड़ा हो गया। यह रात केवल एक प्रदर्शन नहीं थी, यह एक आक्रोश, एक आवाज़ थी जो लोकतंत्र के लिए खड़ी हो रही थी। काव्या के दिल में एक ताजगी सी दौड़ रही थी, जैसे यह आंदोलन सिर्फ़ उसके विचारों का ही नहीं, बल्कि उसके दिल के एक गहरे हिस्से का भी बयान हो। वह जानती थी कि ये रात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ से या तो कोई समाधान निकलेगा, या फिर एक नई उलझन के रूप में यह उसे छोड़ देगी।
काव्या इस आंदोलन का अहम हिस्सा थी। वह एक ओर से विचारधारा की बुलंद आवाज़ थी, जो कभी भी चुप नहीं रहती थी। उसके लिए यह केवल प्रदर्शन नहीं था, यह उसकी जिंदगी का हिस्सा था—जो उसने कई सालों से अपने भीतर दबा रखा था। वह यकीन करती थी कि असहमति लोकतंत्र का गहना है, और अगर इसे दबाया गया तो समाज की आत्मा मर जाएगी। वहीं, अमन, जो पहले कभी इन आंदोलनों से दूर रहता था, आज एक अलग भूमिका में था। उसकी आँखों में पहले जैसा विश्वास नहीं था, लेकिन इस रात की महत्ता को वह भी समझ रहा था। उसने अपनी राजनीतिक विचारधारा में बदलाव नहीं किया था, पर काव्या की भावना और उसकी लड़ाई का समर्थन किया था, क्योंकि वह मानता था कि विरोध का अधिकार सबको होना चाहिए। वह भी यहाँ था, मगर किसी अलग कारण से—नफरत और प्यार, दोनों के बीच खींचतान महसूस करते हुए।
रात गहराई पकड़ने लगी थी, और जंतर मंतर की धरती पर हलचल बढ़ गई थी। प्रदर्शनकारी छात्रों की आवाज़ें गूंज रही थीं, नारे लग रहे थे, और पुलिस ने भी अपनी तैनाती शुरू कर दी थी। अचानक, हलचल बढ़ गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। काव्या की आँखों में गुस्सा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने विचारों से भागने वाली नहीं थी। तभी, एक तेज़ धक्का लगा और काव्या गिरते-गिरते बची, लेकिन तभी अमन की मजबूत पकड़ ने उसे सहारा दिया। वह झिझकते हुए बोला, “तुम ठीक हो?” काव्या ने तर्कपूर्ण अंदाज़ में कहा, “यह सही नहीं है, हमें अब भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।” और वह उसके हाथ से निकलकर आगे बढ़ गई। अमन ने उसे नज़रें फेंकी, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। उसकी आँखों में एक शांत विश्वास था, जैसा वह हमेशा से ही दिखाता था। लेकिन इस रात ने दोनों को किसी न किसी रूप में बदल दिया था।
आंदोलन की रात अब अपनी चरम सीमा पर थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, और विद्यार्थी भागते हुए सड़क पर इधर-उधर दौड़ने लगे। काव्या एक मोर्चे पर खड़ी थी, अमन भी उसके पास था। वह एक-दूसरे के पास थे, लेकिन दोनों के बीच की दीवार अब और भी मजबूत हो गई थी। काव्या के चेहरे पर गुस्सा था, और अमन की आँखों में सवाल—क्या यह रास्ता सच में सही है? क्या इस तरह से लड़ाई जीतने की कोई संभावना है, या फिर यह सिर्फ़ एक मृगतृष्णा है? काव्या ने नज़रे उठा कर उसे देखा, फिर बोली, “तुम्हें समझ नहीं आएगा।” अमन ने शांत स्वर में कहा, “मैं समझता हूँ, पर क्या यह तरीका सही है?” काव्या ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसका दिल अब भी आंदोलन की आग में जल रहा था, और वह जानती थी कि अब उसकी आवाज़ कभी नहीं मानी जाएगी अगर वह चुप बैठती।
आखिरकार, जब पुलिस ने सभी को हटाना शुरू किया, और सड़कों पर बिखरे हुए लोग इधर-उधर भागने लगे, काव्या और अमन एक-दूसरे के पास खड़े थे। भीड़ में जहाँ सन्नाटा था, वहीँ दोनों के बीच एक समझदारी की खामोशी छाई थी। उस रात दोनों के दिलों में एक गहरी बात थी, जिसे उन्होंने बिना कहे समझ लिया था। काव्या ने धीरे से अमन से कहा, “यह सब कुछ बेकार है, क्या हम कभी जीत पाएंगे?” अमन ने सिर झुका लिया और जवाब दिया, “जब तक तुम लड़ती रहोगी, तब तक हम कभी हार नहीं सकते।” उस रात जंतर मंतर पर दोनों के बीच की दीवारें और भी पतली हो गईं, लेकिन सवाल फिर भी बने रहे—क्या विचारधारा और मोहब्बत, दोनों एक साथ चल सकते हैं? क्या काव्या और अमन की लड़ाई एक साथ चल पाएगी, या यह आंदोलन उनके दिलों को हमेशा के लिए दूर कर देगा? उस रात का उत्तर, उस समय किसी के पास नहीं था।
अध्याय ६
जंतर मंतर की वह रात अब अख़बारों की सुर्खियों में थी—“छात्रों पर लाठीचार्ज”, “देशद्रोही नारेबाज़ी या लोकतांत्रिक अधिकार?” जैसी हेडलाइंस टी.वी. चैनलों और सोशल मीडिया पर झूल रही थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस सुबह से ही गरमा गया था। चारों ओर जांच कमिटी की चर्चाएं, मीडिया की आँखें, और छात्र संगठनों के बीच तकरार। अमन को कुछ खबर नहीं थी कि उसका एक फुटेज वायरल हो चुका है—जिसमें वह काव्या के हाथ को थामे उसे बचा रहा है, और पीछे पोस्टर में ‘असहमति देशद्रोह नहीं है’ लिखा है। अगले दिन उसके संगठन के लोग उससे सवाल करने लगे—“तू वहाँ क्यों था?”, “उनके साथ क्यों खड़ा था?”, “क्या अब तू भी राष्ट्र-विरोधियों में शामिल है?” अमन, जो हमेशा से शांत और संतुलित रहा था, पहली बार अपने भीतर खुद से लड़ रहा था। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात की खामोशी उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी।
दूसरी ओर काव्या भी अपनी ही विचारधारा के घेरे में कैद हो गई थी। सोशल मीडिया पर उसे एक खास नेता के करीबी छात्र के साथ देखने पर कई टिप्पणियाँ हो रही थीं—”सिस्टम से मोहब्बत?”, “तू अब हमारे लिए नहीं रही।” फरहा ने उसे समझाने की कोशिश की—“लोग कहेंगे, पर क्या तू अपने दिल की सुन पाएगी?” लेकिन काव्या अब खुद से भी सवाल कर रही थी—क्या उसकी लड़ाई अब भी साफ़ है? क्या अमन उसके संघर्ष की समझ रखता है या वह सिर्फ उसकी नज़दीकी का फायदा उठा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल—क्या दोनों एक-दूसरे के विचारों से लड़ते-लड़ते अब खुद को ही खोने लगे हैं? प्रोफेसर सुरभी सेन ने दोनों को बुलाया, अलग-अलग, और उनसे सिर्फ़ एक ही बात कही—“सवाल पूछना मत छोड़ना, लेकिन इतना ज़रूर सोचो—क्या तुम्हारे सवाल तुम्हारे प्यार से बड़े हैं?”
इस माहौल में दोनों एक-दूसरे से दूरी बना बैठे, पर एक-दूसरे की गैरमौजूदगी हर दिन चीखती रही। कैंपस में अब दोनों का आमना-सामना कम होता था, और अगर होता भी, तो नज़रों की पुरानी पहचान अब झिझक में बदल गई थी। एक दिन अमन ने अपनी डायरी में लिखा—”उसने मुझे समझना नहीं चाहा, शायद मैं समझाया भी नहीं। पर क्या रिश्ते तर्क से चलते हैं?” उसी शाम काव्या ने अपनी नोटबुक में लिखा—”उसने मेरा हाथ उस रात थामा था, पर क्या वो मेरी आवाज़ को थाम पाया?” उस समय दोनों को शायद ये एहसास नहीं था कि विचारधाराओं के नाम पर पूछे गए ये सवाल अब विचार नहीं, रिश्तों की परीक्षा बन चुके हैं। और जब मोहब्बत के सामने सवाल खड़े हो जाएँ, तब जवाब कहीं भीतर से ढूंढने पड़ते हैं—कभी अकेले, कभी बहुत चुपचाप।
अध्याय ७
जंतर मंतर की रात को एक महीना बीत चुका था, लेकिन उसका असर अभी भी अमन और काव्या के बीच सांस ले रहा था—ठीक वैसे जैसे धूप में छिपा हुआ धुंआ, जो दिखता नहीं पर फेफड़ों को धीरे-धीरे भरता चला जाता है। कैंपस अब धीरे-धीरे चुनावी रंगों से रंगने लगा था। हर संगठन नए चेहरों के साथ मैदान में उतर रहा था, और पुराने चेहरों से उम्मीदें लगाई जा रही थीं। अमन को संगठन ने छात्रसंघ सचिव पद के लिए नामांकित कर दिया था—उसके सोच-समझ, संतुलित भाषा और ‘ज़मीन से जुड़े’ व्यक्तित्व के कारण। लेकिन नामांकन के दिन वह चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा, कैंडिडेसी फॉर्म भरने की बजाय अपनी पुरानी डायरी को घूरते हुए। दूसरी ओर, काव्या को लगा जैसे उसे अमन का साथ एक अस्थिर भरोसे की तरह छोड़ रहा है। वह चुपचाप फरहा से बोली—“शायद, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, वह हमारी लड़ाई का साथी नहीं बन सकता।” फरहा ने सिर्फ़ इतना कहा, “या शायद, मोहब्बत किसी विचारधारा से बड़ी नहीं, बस अलग होती है।”
अमन और काव्या के बीच अब मुलाकातें कम थीं, और जब होतीं, तो सन्नाटे में भी गूंज होती थी। एक दिन, जब दोनों लाइब्रेरी के गलियारे में टकराए, नज़रों ने कोशिश की, पर शब्द नहीं निकले। आखिरकार, अमन ने ही हिम्मत जुटाकर कहा—“मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।” वे दोनों पीपल के उस पेड़ के नीचे जा बैठे जहाँ कभी पहली बार उन्होंने कविता पर बहस की थी। काव्या की आँखों में आंसुओं की नमी थी, लेकिन आवाज़ सख्त थी—“क्या बात करनी है? यह कि अब तुम्हें मेरी सोच से दिक्कत होने लगी है? या कि तुम्हारे संगठन ने तुम्हें ये कह दिया है कि मैं तुम्हारी राह में बाधा बन रही हूँ?” अमन ने गहरी सांस ली और कहा—“मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, काव्या। तुम्हारे साथ होते हुए मुझे लगता है कि मैं किसी और की दुनिया में घुस आया हूँ—जहाँ हर बात को साबित करना पड़ता है। और तुम्हारे साथ न रहकर, लगता है जैसे खुद से जुदा हो गया हूँ।” काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली—“मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि तुम समझो कि मैं क्यों लड़ती हूँ।”
उस शाम पेड़ के नीचे बैठे-बैठे दोनों ने अपने अंदर के डर, ग़लतफहमियाँ और अहंकार को देखा—जैसे आईना हो, जिसमें उनका प्यार थोड़ा धुंधला, पर अब भी ज़िंदा दिख रहा था। लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी उभर रही थी—कि दोनों के रास्ते शायद एक-दूसरे के समानांतर तो चल सकते हैं, लेकिन संग नहीं। काव्या ने कहा, “हम बहस करते हैं तो लगता है एक नई सोच जन्म लेगी, लेकिन फिर दिल चुपचाप पीछे छूट जाता है। क्या तुम दिल से बहस कर सकते हो?” अमन ने धीरे से कहा, “शायद नहीं। मैं तर्कों से बना हूँ, और तुम—तुम आग हो।” फिर दोनों खामोश हो गए, जैसे कोई फैसला दोनों के बीच बैठा हो, और वह अब न कोई नारा था, न कोई प्रस्ताव—बस एक स्वीकार।
कैंपस में चुनावी दिन आ गया। अमन ने आख़िरी समय में कैंडिडेसी वापस ले ली। लोगों ने तरह-तरह की बातें कीं—किसी ने कहा डर गया, किसी ने कहा कन्फ्यूज़ है, किसी ने आरोप लगाया कि वामपंथी मोहब्बत ने उसे पिघला दिया। लेकिन अमन जानता था, उसने मोहब्बत को चुना भी नहीं, छोड़ा भी नहीं—बस समझा। काव्या ने आंदोलन के मंच पर भाषण दिया, उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वैसा ही जुनून। उसके भाषण के आख़िरी शब्द थे—“हम लड़ेंगे, क्योंकि सवाल अब भी ज़िंदा हैं। और मोहब्बत अगर सच्ची है, तो वह इन सवालों से डरती नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलती है।” हॉल में तालियाँ गूंजी, और पीछे खड़ा अमन, उन तालियों में नहीं, पर उसकी नज़रों में था।
इस अध्याय का अंत कोई पूर्ण विराम नहीं था—यह एक अल्पविराम था, जहाँ विचारधारा और दिल, दोनों को सांस लेने का वक्त मिला। और दोनों जान चुके थे कि मोहब्बत और विचार, साथ चल सकते हैं—अगर दोनों एक-दूसरे को खत्म करने की नहीं, समझने की कोशिश करें।
अध्याय ८
ठंडी हवा अब दिल्ली की शामों में घुल चुकी थी। नवंबर की हल्की धुंध हर शाम को एक पुरानी याद की तरह ढँक देती थी। एक साल बीत चुका था उस रात को — जंतर मंतर की, बहसों की, आंसुओं और चुप्पियों की रात। काव्या अब एम.ए. की अंतिम सेमेस्टर में थी, और कैंपस की सबसे तेज़ आवाज़ों में गिनी जाती थी। अमन यूनिवर्सिटी से निकल चुका था, लेकिन दिल्ली को कभी पूरी तरह छोड़ा नहीं। उसने इतिहास में रिसर्च करना शुरू किया था, लेकिन उसकी डायरी में अब भी कुछ पन्ने अधूरे थे — काव्या के नाम लिखे गए, कभी भेजे नहीं गए। वह आज भी दिल्ली की सड़कों पर चलता हुआ खुद से टकराता रहता था। और फिर एक दिन, खबर आई — एक साल पूरे होने पर उसी आंदोलन की याद में एक ‘स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जंतर मंतर पर।
काव्या ने तय कर लिया, वह जाएगी। उसे नहीं पता था कि वहाँ कौन आएगा, क्या होगा, लेकिन वह उस रात को फिर से जीना चाहती थी — सवालों की तरह अधूरी रह गई बातों को महसूस करने के लिए। वह जब वहाँ पहुँची, तो भीड़ थी, नारे थे, मोमबत्तियाँ थीं — लेकिन पहले जैसी नहीं, अब सब कुछ संयत था, समझदारी से भरा। वह कुछ दूर जाकर चुपचाप बैठ गई, तभी उसे एक जानी-पहचानी आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा — अमन खड़ा था, वही पुराना बैग, वही किताबों से झांकती आँखें, लेकिन अब थोड़ी नरम, थोड़ी थकी हुई। दोनों ने एक-दूसरे को देखा, और बिना कुछ कहे पास आ बैठे। कुछ पल खामोश बीते, फिर अमन ने धीरे से कहा, “मैं जानता हूँ, हम अलग थे। हम आज भी हैं। लेकिन उस रात जो था… वो मैंने कभी नहीं भुलाया।” काव्या ने मुस्कराकर उसकी तरफ देखा, “वो रात मेरी आवाज़ में अब भी जिंदा है… और शायद तुम्हारे खामोशियों में भी।”
धीरे-धीरे बातें खुलने लगीं — इस बार बहस नहीं, सिर्फ़ स्वीकार। काव्या ने कहा, “मैं अब भी लड़ती हूँ, हर रोज़। लेकिन अब मुझे ये एहसास है कि लड़ाई सिर्फ़ मंच पर नहीं, दिल के भीतर भी होती है।” अमन ने जवाब दिया, “और मैंने सीखा है कि हर सवाल का जवाब ‘हाँ’ या ‘ना’ में नहीं होता। कुछ सवाल सिर्फ़ साथ बैठकर सुने जा सकते हैं।” दोनों की आँखों में अब कोई जीतने की चाह नहीं थी, न ही कोई हार का डर — बस एक सहज साथ, जैसे दो नदियाँ जो अलग-अलग दिशा में बहती हैं, लेकिन कभी-कभी एक घाट पर रुककर एक-दूसरे का पानी छू लेती हैं।
रात गहराती गई। मोमबत्तियाँ बुझने लगीं। आस-पास के चेहरे धीरे-धीरे लौटने लगे। अमन और काव्या भी उठे। जंतर मंतर की सीढ़ियों से उतरते हुए काव्या ने धीमे से कहा, “हम फिर मिलेंगे?” अमन ने बिना रुके जवाब दिया, “अगर हमारी लड़ाइयाँ ईमानदार रहेंगी, तो हाँ।” फिर एक क्षण चुप रहकर उसने जोड़ा, “और अगर हमारी मोहब्बत ने इंतज़ार करना सीखा, तो ज़रूर।” वे दोनों अलग दिशाओं में चले गए — कोई फिल्मी विदाई नहीं, कोई रोती आवाज़ नहीं — बस एक समझ, एक वादा, उस रात का वादा।
दिल्ली की वो सर्द हवा उस रात भी बह रही थी — वही जंतर मंतर, वही सड़कें, लेकिन अब वे दो लोग बदल चुके थे। अब वे सिर्फ़ विरोधी विचारधाराओं के प्रतिनिधि नहीं थे, वे उस पीढ़ी का हिस्सा थे जिसने सीखा था कि प्यार और असहमति दोनों साथ रह सकते हैं — अगर दिल और दिमाग एक-दूसरे को सुनना चाहें। और इस बार, जंतर मंतर पर कोई नारा नहीं गूंजा — सिर्फ़ दो दिलों की खामोशियाँ थीं, जो शायद सबसे बड़ी क्रांति बन सकती थीं।
***